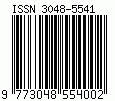Archives
-
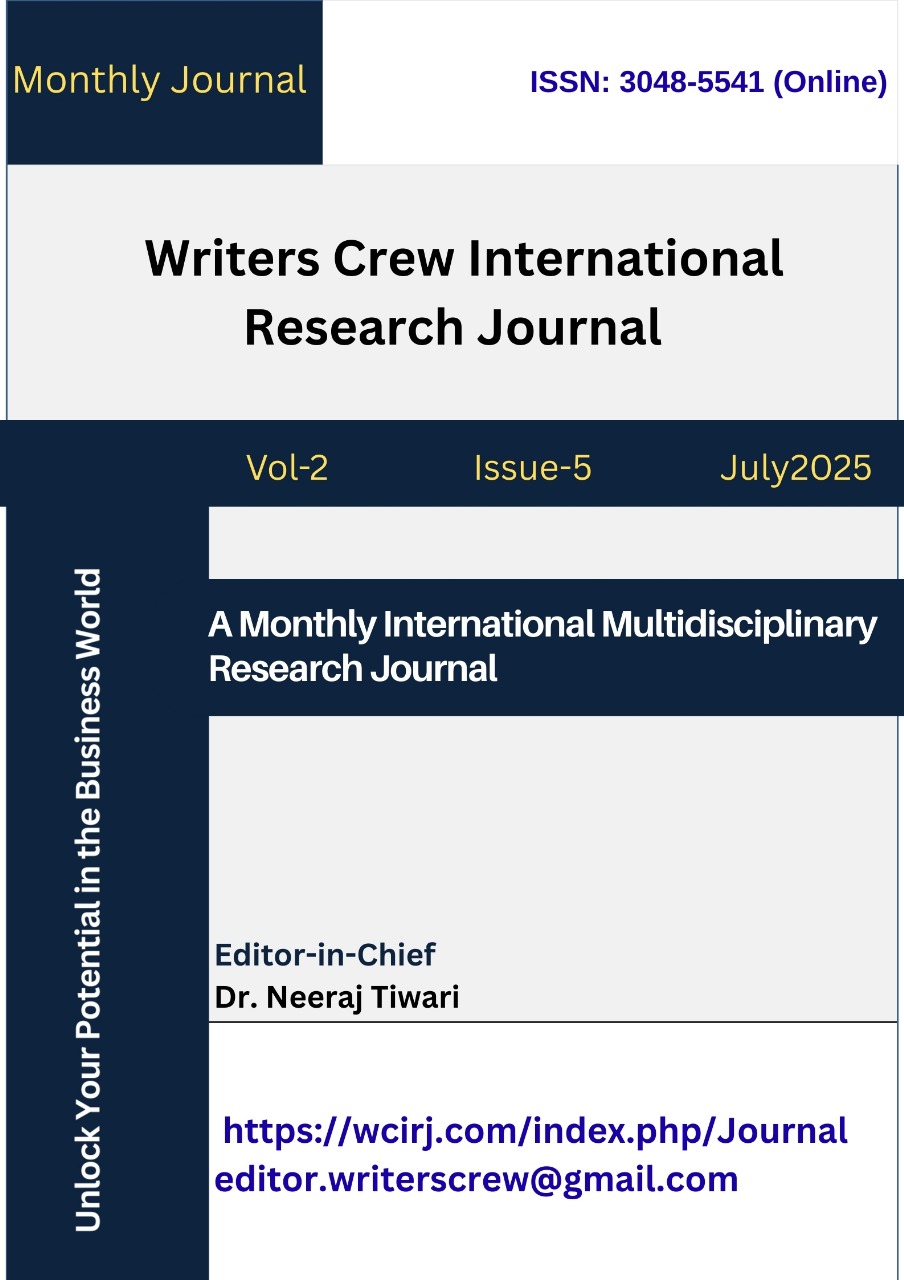
प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा: बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता के परिपेक्ष्य में एक दृष्टिकोण
Vol. 2 No. Issue: 5, July, 1524-1535 (2025) (2025)सार
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं, आवश्यकताओं एवं भिन्नताओं के बावजूद, समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण शैक्षिक चुनौती के रूप में उभर रही है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं तथा शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा आँकड़ों का संकलन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं संबंधित अभिलेखों के माध्यम से किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त शैक्षिक संसाधनों, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों, सहयोगी सेवाओं तथा सकारात्मक विद्यालयी वातावरण की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी पाया गया कि सीमित संसाधन, शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी तथा जागरूकता का अभाव समावेशी शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। अतः यह अध्ययन सुझाव देता है कि प्राथमिक स्तर पर बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को सफल बनाने हेतु नीति-निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक सहभागिता तथा विद्यालयी संसाधनों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
बीज शब्द: समावेशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता, दिव्यांग बच्चे, शिक्षक प्रशिक्षण
-
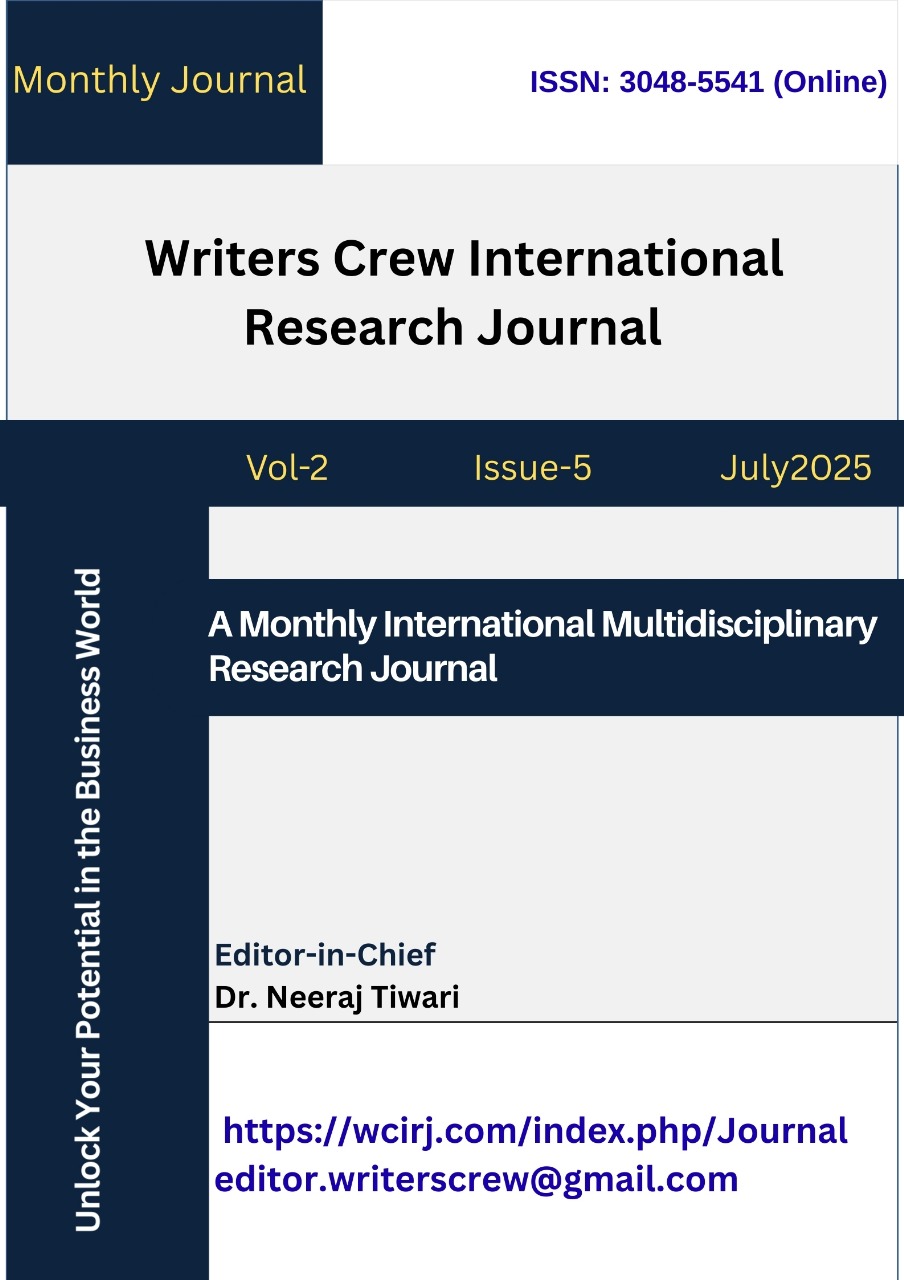
Women’s Property and Inheritance Rights under the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005: A Critical Legal and Socio-Empirical Analysis
Vol. 2 No. Issue: 5, July, 1513-1523 (2025) (2025)Abstract
The research study summarises that the reformation in the
legal notions of the Hindu Succession Act or HSA, 2005,
is recognised as a progressive hallmark towards women's
empowerment, zero gender discrimination, and gender
equality in Indian society. The study objective is to
thoroughly scrutinise the influence of HSA 2005, upon
women's rights and empowerment. This research study
followed the secondary data collection method with
thematic interpretations. The key finding associates with
inheritance lawsuits and constitutional paradigms of nondiscrimination and equality. This study revealed the gap
between substantive social justice and formal legal
equality in terms of gender equality from the Indian
perspective. Despite having sociocultural resistance, the
Indian judicial interpretations have legally strengthened
the legal position and rights of a daughter upon her
father's ancestral properties.
Keywords: Inheritance Law, the Hindu Succession Act,
Gender Equality, Women’s Property Rights, Feminism
Theory -
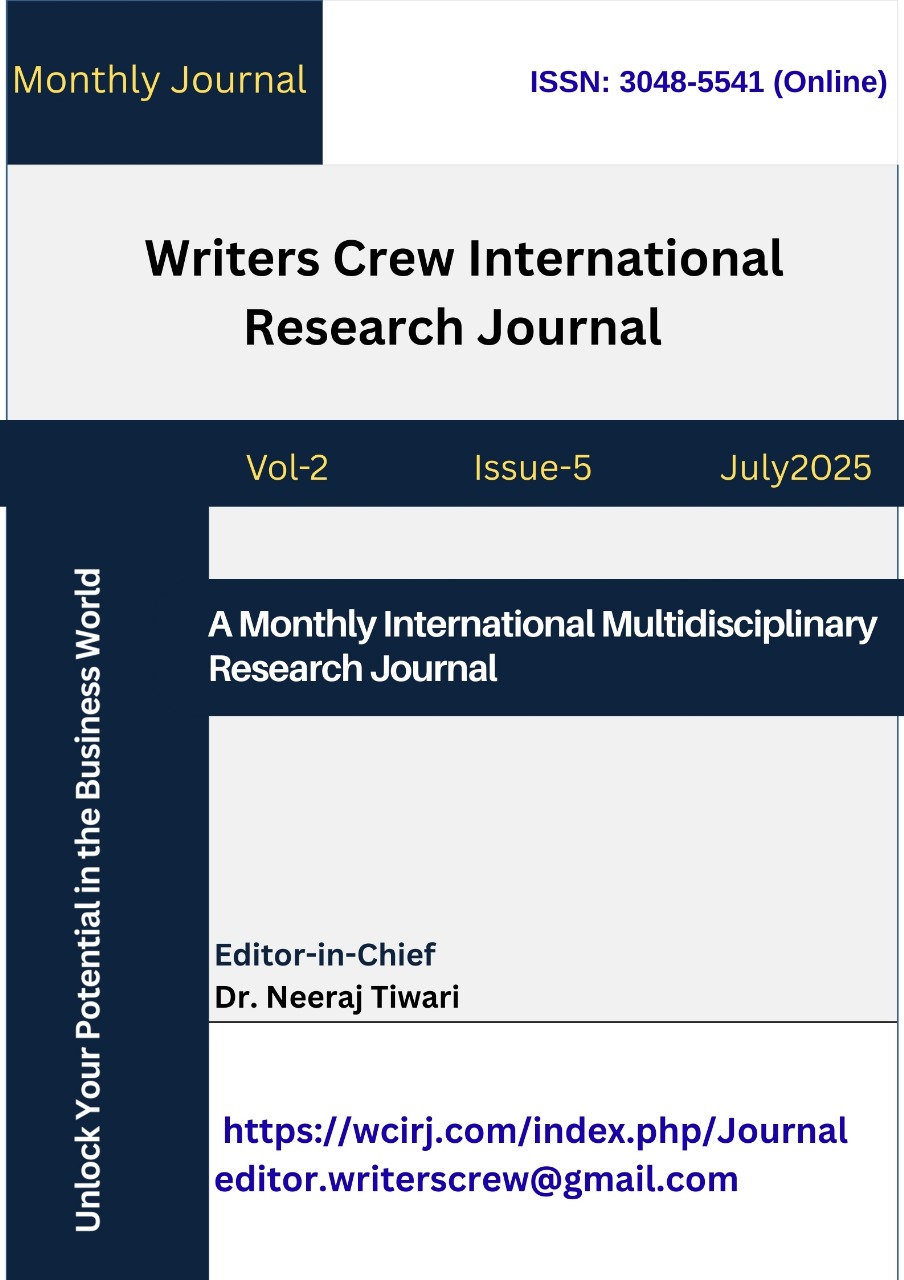
An Exploratory Study of Trade Union Rights and Their Influence on Collective Bargaining Outcomes in Modern Employment Environments
Vol. 2 No. Issue: 5, July, 1503-1512 (2025) (2025)Abstract
The context of the current research paper highlights the
types of Trade Union Rights and their influence on the
bargaining towards wage structure, duty hours, and a secure
job & work atmosphere through a collective voice. The key
objectives of the research study ensure the historical
evaluation of the Trade-Union-Act, 1956, from an Indian
perspective. This study followed the secondary data
collection method, doctrinal analysis, and thematic
interpretations to make a credible solution, aligned with
predefined objectives. The main findings outline that the
internal coordination error, funding unavailability, and
perspective variations are the key reasons for not providing
equal rights scope for the staff in modern workplaces. This
study finally claims that reshaping Indian Labour Law
generates safer and sustainable industrial democracy across
national and international levels.
Keywords: Collective Bargaining, Industrial Relations,
Trade Union, Indian Labour Law, Trade Union Act -
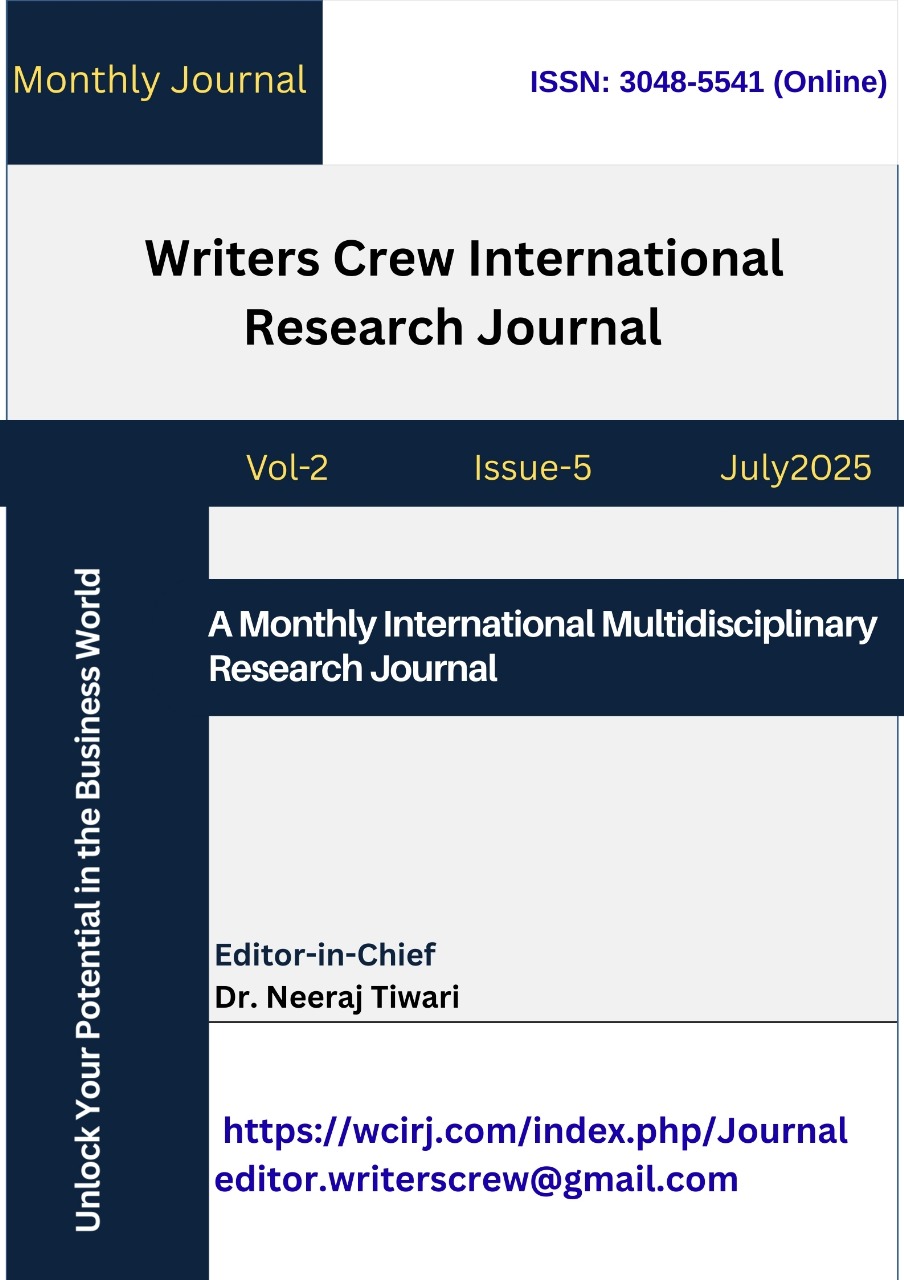
CHALLENGES FACED BY RURAL STUDENTS IN LEARNING TO SPEAK ENGLISH
Vol. 2 No. Issue: 5, July,page ,1489-1502 (2025)
-
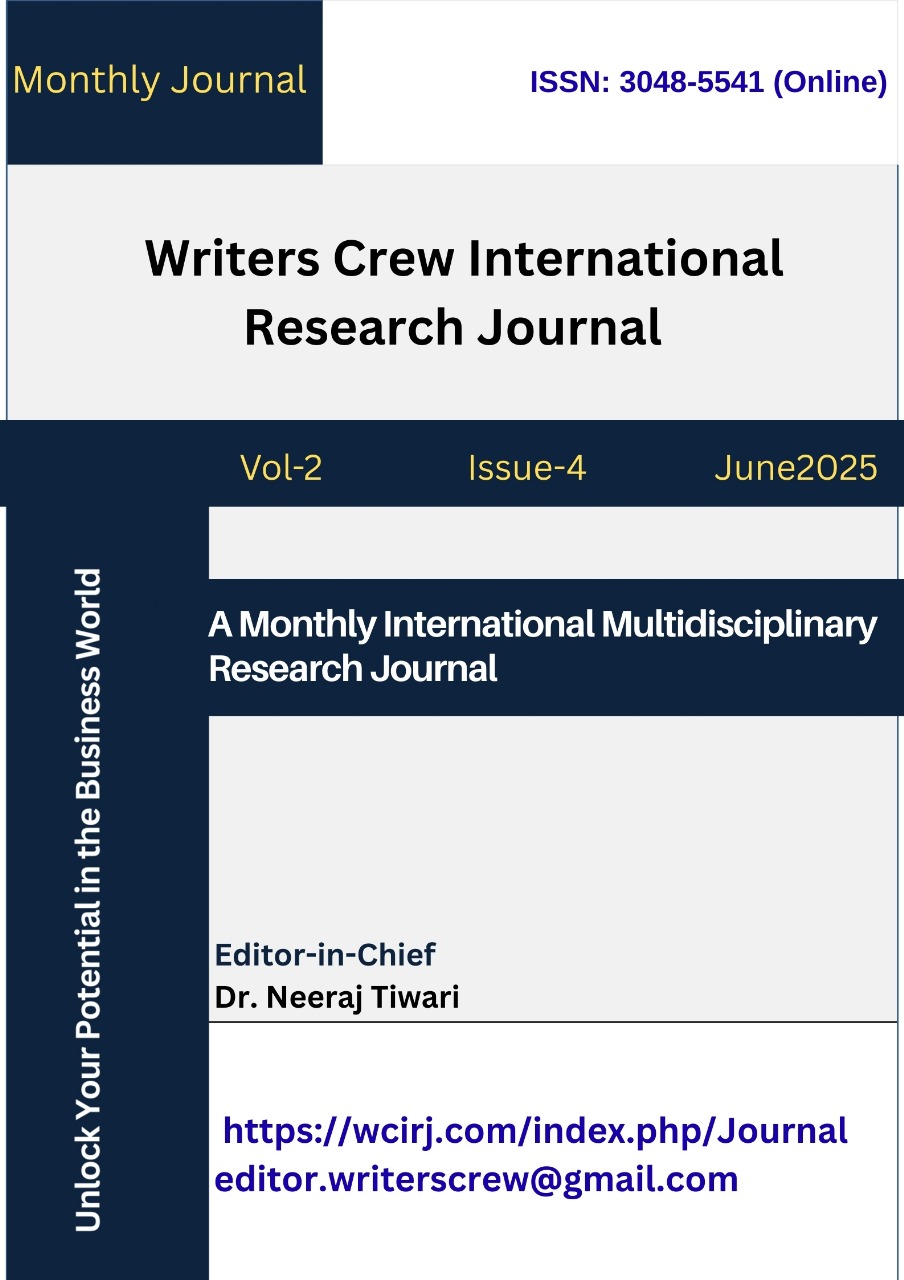
Role of Technology in Modern Classrooms A Shift from Chalkboard to Smartboard
Vol. 2 No. Issue: 4, June, pg. 1468-1488 (2025)Abstract
This research is aimed at identifying the intermingling factor of technology in the contemporary
classroom with particular attention to the paradigm shift between traditional chalkboards and
smartboards in the classrooms. Therefore, the primary research question will be the assessment
of the impact of digital tools on student engagement, the effectiveness of instruction, and the
overall quality of pedagogy. The study will use secondary research model and critically evaluate
chosen institutional and scholarly literature to reveal emerging trends in the permeation of
technology in the educational setting. Empirical research findings indicate that digital
technologies have improved the interactivity in the classroom, resulted in active learning and
facilitated greater efficiency of instruction. Smartboards and the associated technology tools are
gradually being incorporated as an element of the teaching arsenal of instructors and thus recast
what was previously a fundamentally unidirectional pedagogical practice, to become more
socially interactive and participatory. However, the extent of these positive impacts is dependent
on factors such as teacher quality, availability of technological resources and institutional
investment. Accordingly, the research begins with the assumption that technology is a
transformative force in pedagogy today and calls for further empirical research that will help to
understand the long-term consequences of its implementation in relation to learning and
educational equity.
Keywords: Technology, Chalkboard, Smartboard, Classrooms -
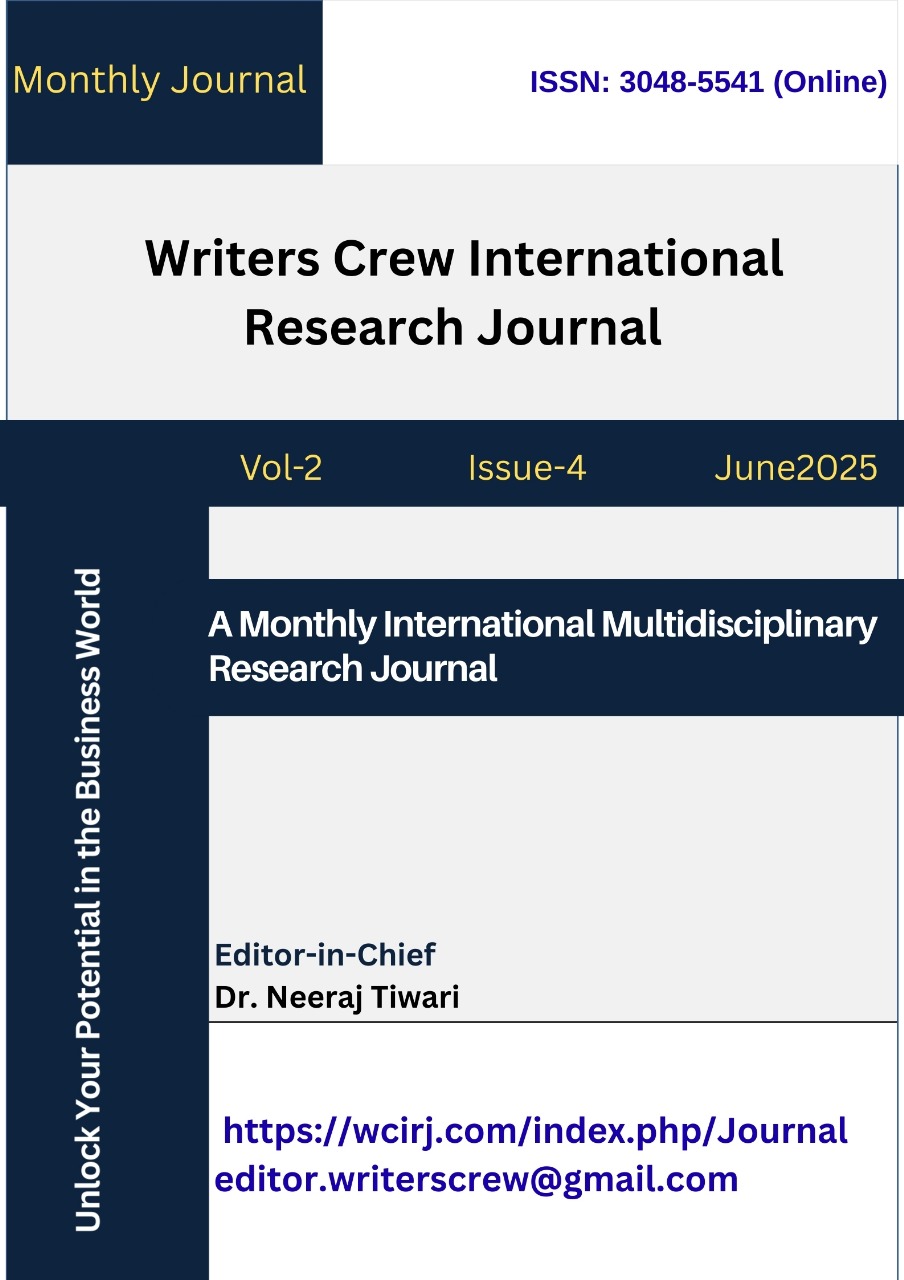
The role of technology in creating inclusive learning environments
Vol. 2 No. Issue: 4, June, pg. 1453-1467 (2025) (2025)Abstract
This analysis examines how technology can be useful in designing all-inclusive learning
spaces that support the integration of diverse learners and advance the idea of equitable access to
education. The key aim is to study the role played by digital tools, assistive technologies, as well
as institutional strategies in ensuring inclusivity in education and grasp the challenges that render
their successful application a challenge. The qualitative research design was taken, and
secondary data has been collected by using the peer-reviewed journals, institutional reports, and
policy documents published between the years 2020 and 2025. Thematic analysis was applied to
data to reveal important insights and patterns. The results indicate that technology improves
accessibility to students with disabilities, promotes personalized learning with the help of
adaptive learning systems, and encourages teamwork in online classrooms. Yet, nothing has
replaced inclusivity because of barriers that include incompetent teacher training, infrastructural
inequality, and inconsistent policy structures. The researchers conclude that technology
potentially has a great possibility to democratize education, but to be able to fully realize
inclusion, technological innovations, professional development, and fair implementation of
policies should be integrated.
Keywords: Inclusive Learning, Digital technology, Learners. -
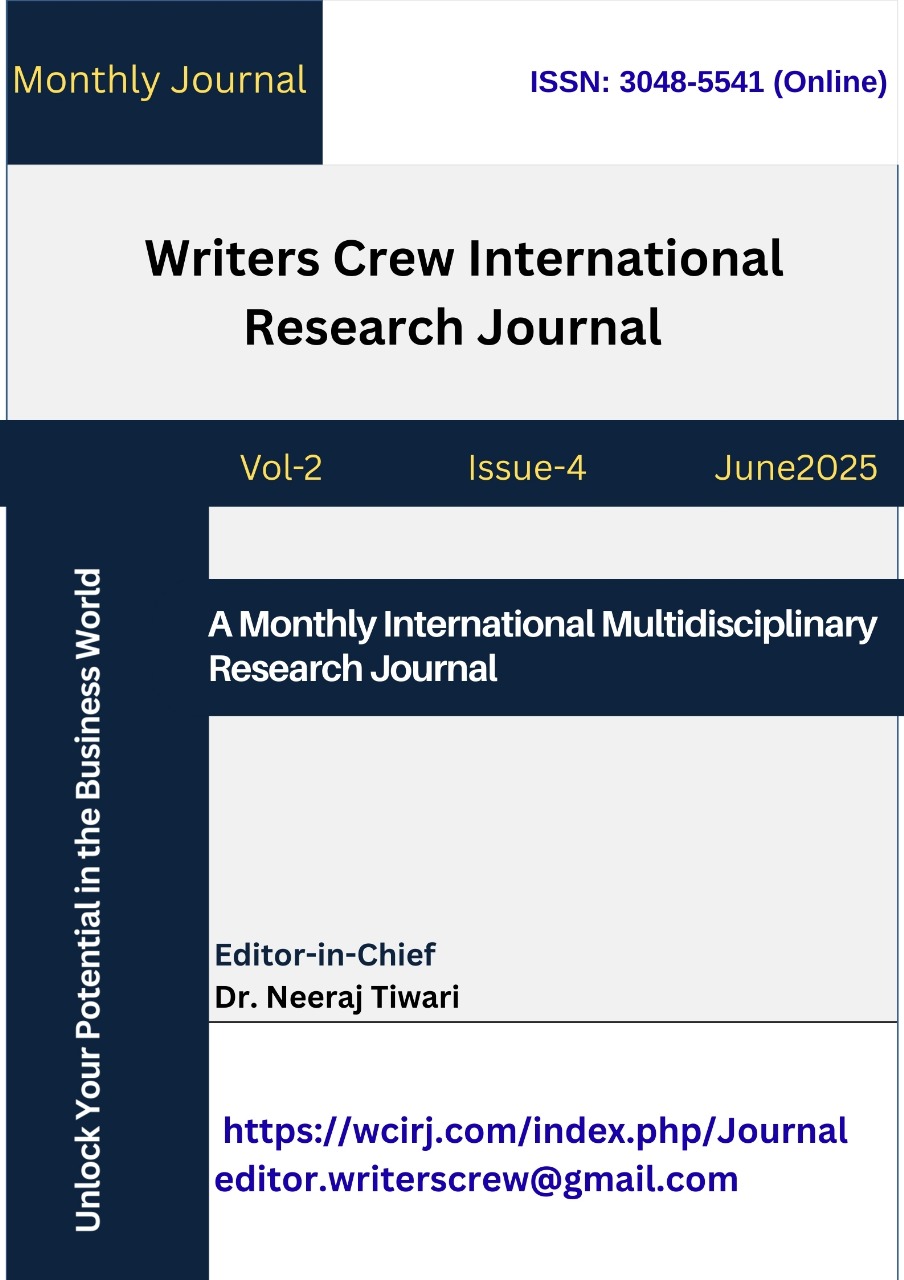
तनाव निवारण में योग और पंचकर्म की उपचारात्मक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन
Vol. 2 No. Issue: 4, June, pg. 1419-1452 (2025) (2025)सारांश
यह अध्ययन तनाव निवारण में योग और पंचकर्म की उपचारात्मक प्रभावशीलता का तुलनात्मक विश्लेषण है। आधुनिक जीवनशैली में तनाव की व्यापकता ने स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे निपटने के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक एवं योगिक उपायों का महत्व बढ़ रहा है। इस शोध का उद्देश्य योग और पंचकर्म के माध्यम से तनाव से राहत पाने के प्रभाव का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। अध्ययन में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को चुना गया, जिन्हें अलग-अलग समूहों में बाँटा गया। एक समूह को योग उपचार दिया गया, दूसरे समूह को पंचकर्म उपचार, और तीसरे समूह को नियंत्रण के रूप में सामान्य जीवनशैली का अनुसरण करने दिया गया। शोध के दौरान, तनाव स्तर मापने के लिए मानक मापदंड एवं प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि दोनों ही उपचार पद्धतियों ने तनाव स्तर में उल्लेखनीय कमी की, किंतु पंचकर्म ने योग की तुलना में अधिक प्रभावी परिणाम दिखाए। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि योग एवं पंचकर्म दोनों ही तनाव निवारण में प्रभावकारी हैं, किंतु पंचकर्म अधिक तीव्र एवं दीर्घकालिक राहत प्रदान कर सकता है। यह अध्ययन आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा तनाव प्रबंधन में इन पारंपरिक उपचार विधियों के समुचित प्रयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
मूल शब्द - तनाव प्रबंधन, योग और पंचकर्म, आयुर्वेदिक उपचार, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रभाव
-
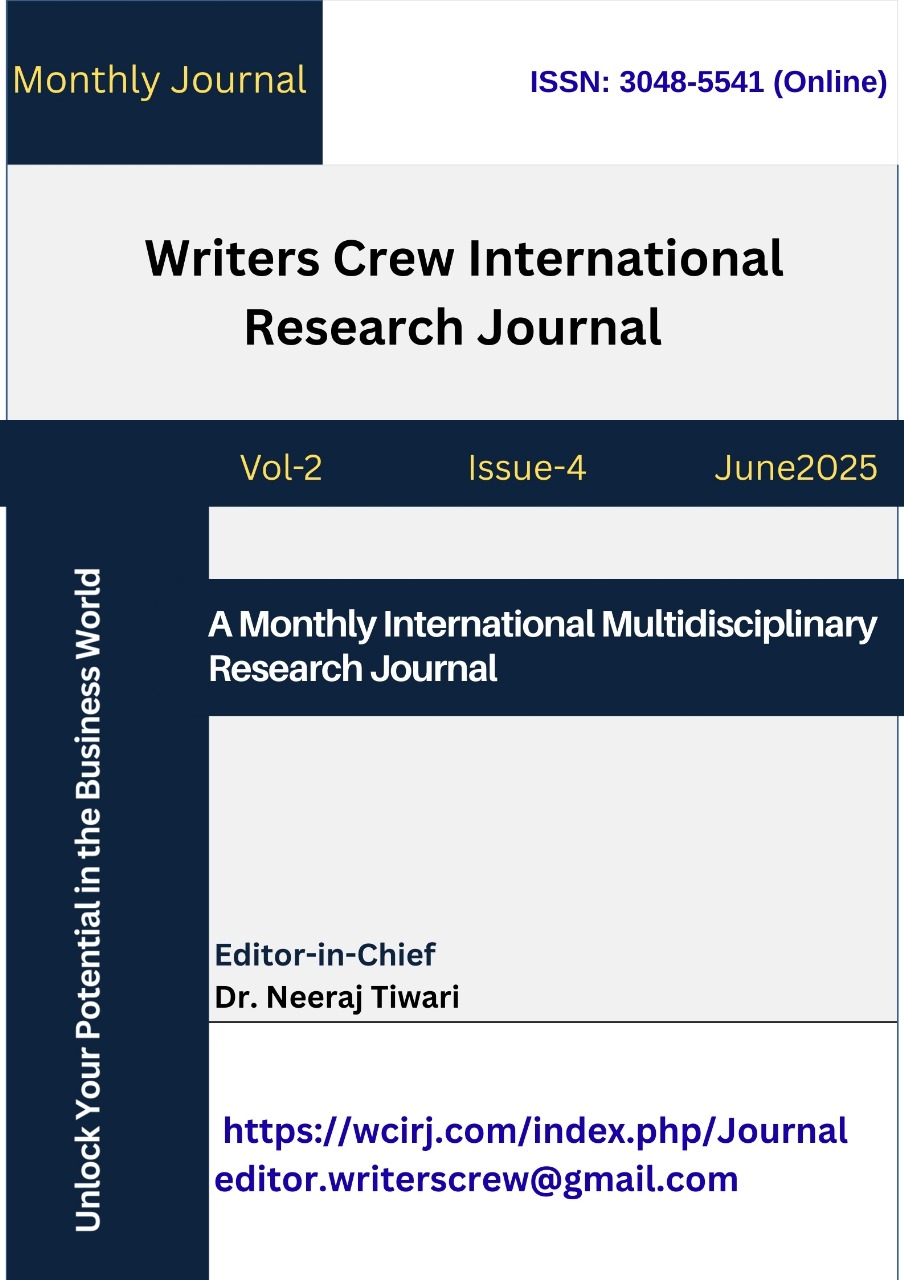
THE DARK SIDE OF AI: INSECURITY, SURVEILLANCE, AND STRESS IN THE ACADEMIC FIELD AMONG STUDENTS AND TEACHERS
Vol. 2 No. Issue: 4, June, pg. 1402-1418 (2025) (2025)Abstract
The study explores the negative psychological and ethical consequences of the application of Artificial Intelligence (AI) in the academic field among students and teachers. Although AI has transformed the education sector to be more efficient, accurate and accessible, its intensive use has raised some fears about job losses, invasion of privacy and even mental health issues among both teachers and learners. The study examines four key themes, including AI-induced job insecurity, AI-enabled surveillance, stress among students, and stress among teachers using such methods as a secondary qualitative approach and thematic analysis. The research is based on the Sociotechnical Systems Theory and the Technology Acceptance Model and presents the impact of automation and continuous digital surveillance on trust, autonomy, and emotional well-being in the learning context. The results indicate that even though AI has led to benefits in terms of economics and operations, it has created professional anxiety, invasion of privacy, and mental stress. The study suggests policies of ethical AI implementation, teacher training on digital literacy and support, privacy rules and measures, and improved mental health services. Altogether, this paper underlines the necessity of a moderate attitude to the use of AI, which should be concerned with both the development of technologies and the well-being of humanity in education.
Keywords: Artificial Intelligence (AI), education, job insecurity, surveillance, stress, mental health.
-
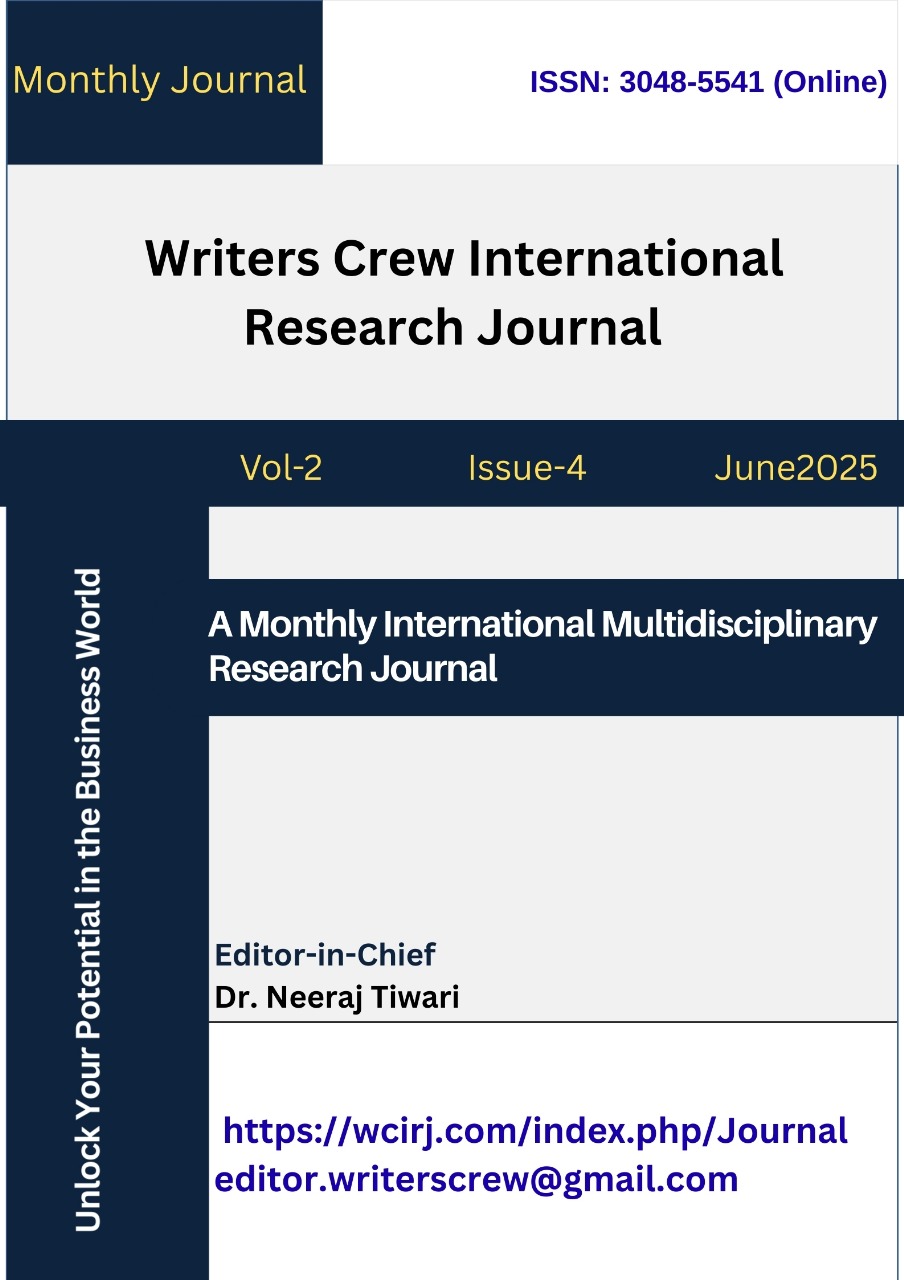
विद्यालय स्तर पर योग के माध्यम से करुणा, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास की संभावनाएँ
Vol. 2 No. Issue: 4, June, pg. 1377-1401 (2025) (2025)सारांश
विद्यालय स्तर पर योग का अध्ययन वर्तमान समय में शैक्षिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यह शोध पत्र इस बात का विश्लेषण करता है कि किस प्रकार योग अभ्यास विद्यार्थियों में करुणा, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मानवीय मूल्यों का विकास कर सकता है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक है। विशेष रूप से, ध्यान, प्राणायाम और योगासन जैसे अभ्यास विद्यार्थियों की आत्मसामंजस्य, आत्मानुशासन और सामाजिक समर्पण की भावना को मजबूत करते हैं। इस अध्ययन में यह पाया गया कि नियमित योग अभ्यास विद्यार्थियों में करुणा और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, जिससे वे अधिक सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। साथ ही, योग के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता भी विकसित की जा सकती है। इस शोध का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर योग के माध्यम से मानवीय मूल्यों का संवर्धन सुनिश्चित करना है, ताकि छात्र एक समावेशी, जिम्मेदार और करुणामयी समाज का निर्माण कर सकें। निष्कर्षस्वरूप, यह अध्ययन योग को शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एवं सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है।
कीवर्ड्स - विद्यालय स्तर, योग और मानवीय मूल्य, करुणा और सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी, मानसिक और भावनात्मक विकास, योगाभ्यास का मूल्यांकन, शिक्षा में योग का समावेशन
-
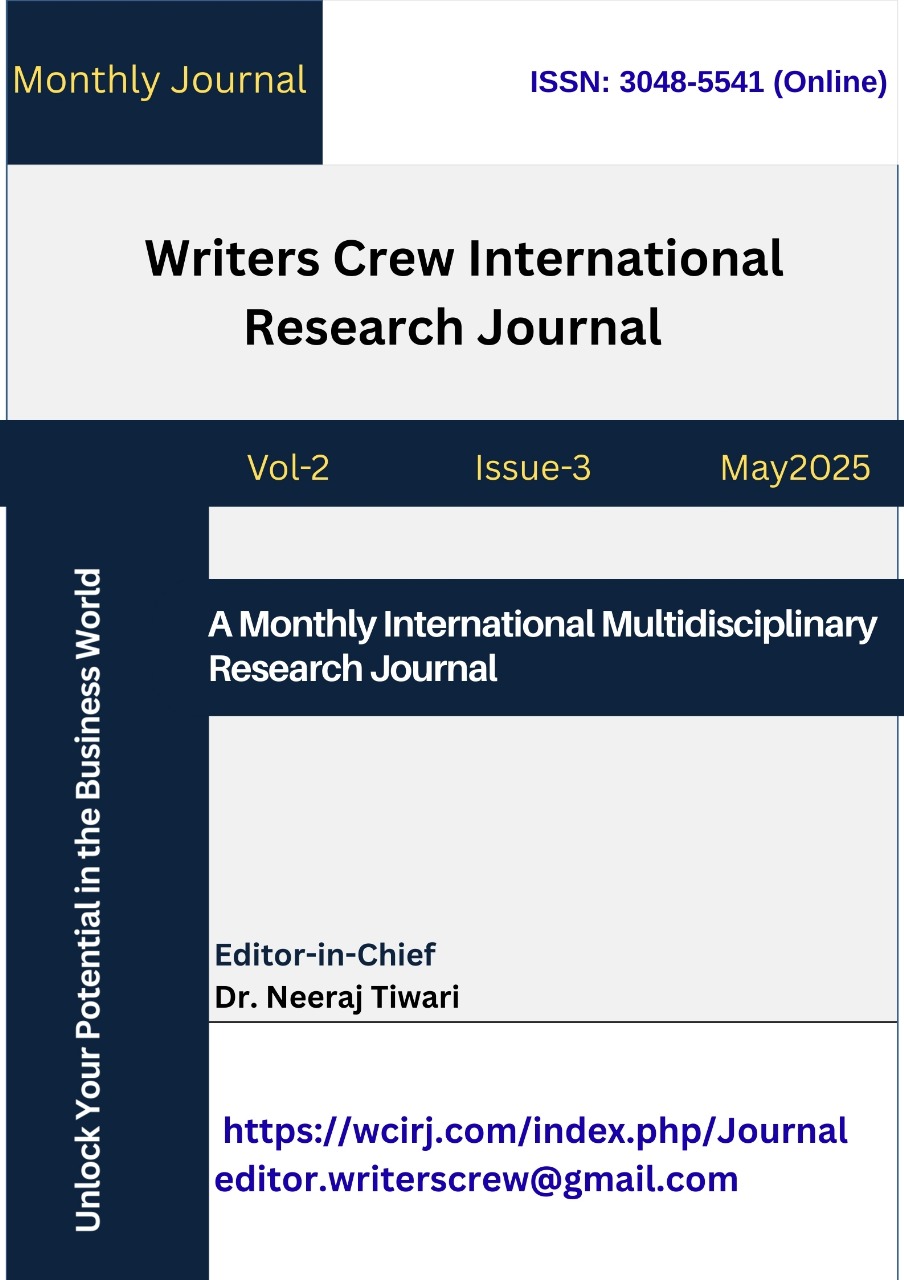
बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में माता-पिता की भागीदारी की भूमिका
Vol. 2 No. Issue: 3, May, pg. 1315-1344 (2025) (2025)सार
बच्चों की शक्षै णिक उपलब्धि को आकार देनेमेंमाता-पिता की भागीदारी महत्वपर्णू र्णभमिू का निभाती है।
माता-पिता प्रथम शिक्षक के रूप मेंकार्य करतेहैंऔर स्कूल की गतिविधियों मेंसक्रिय भागीदारी, गहका ृ र्य
मेंसहयोग, प्रेरणा और घर पर एक अनकुूल शिक्षण वातावरण के निर्माण के माध्यम सेबच्चेके सीखनेके
प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करतेरहतेहैं। यह शोध पत्र बच्चों की शक्षिै क सफलता मेंमाता-पिता की भागीदारी
की बहुआयामी भमिू का का अन्वेषण करता है, भावनात्मक, सामाजिक और शक्षै णिक पहलओु ं सहित
विभिन्न आयामों का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन मौजदा ू साहित्य की समीक्षा करता है,
अनभवजन्य ु निष्कर्ष प्रस्ततु करता है, और सामाजिक-आर्थिकर्थि , सांस्कृतिक और शक्षिै क संदर्भों में
माता-पिता की भागीदारी के निहितार्थों पर चर्चाकरता है।
सारांश इस बात पर ज़ोर देता है कि माता-पिता की भागीदारी कैसे छात्रों की प्रेरणा, उपस्थिति,
आत्म-सम्मान और दीर्घका र्घ लिक शक्षै णिक परिणामों को बढ़ाती है। यह आर्थिकर्थि कठिनाई, शक्षिै क
पष्ठभ ृ मिू की कमी या सीमित समय के कारण माता-पिता के सामनेआनेवाली चनौ ु तियों पर प्रकाश
डालता है, और इन अतरालों ं को पाटनेकी रणनीतियों की खोज करता है। शोध पद्धति चयनित स्कूलों के
माता-पिता, शिक्षकों और छात्रों के सर्वेक्षणों और प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण पर आधारित है। आकं ड़ों कीव्याख्या और तलनात्मक ु विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्ययन माता-पिता के सहयोग और बच्चों की
शक्षै णिक सफलता के बीच मज़बतू सकारात्मक सहसंबंधों की पहचान करता है। निष्कर्ष इस बात पर ज़ोर
देता है कि माता-पिता की भागीदारी शक्षै णिक उपलब्धि का एक महत्वपर्णू र्ण निर्धारक है, और
अभिभावक-विद्यालय साझदारी े को मज़बतू करनेके लिए स्कूल नीतियों और सामदा ु यिक पहलों की
आवश्यकता पर बल देता है।अततः ं , यह अध्ययन शिक्षकों, नीति निर्माताओं और स्वयं अभिभावकों को एक ऐसा वातावरण बनानेके
लिए व्यावहारिक अतं र्दृष्टि प्रदान करता हैजहाँबच्चेशक्षै णिक रूप सेफल-फूल सकें। येनिष्कर्ष न केवल
मौजदा ू विद्वानों की आम सहमति की पष्टि ु करतेहैं, बल्कि सर्वेक्षण की गई आबादी मेंसंदर्भ-र्भविशिष्ट
समझ को भी बढ़ावा देतेहैं।
कीवर्ड
अभिभावक की भागीदारी, शक्षै णिक उपलब्धि, छात्र प्रेरणा, अभिभावक-विद्यालय साझदारी े , शक्षिै क सफलता
Vol. 2, Issue: 3, May, pg. 1315-1344 (2025) -
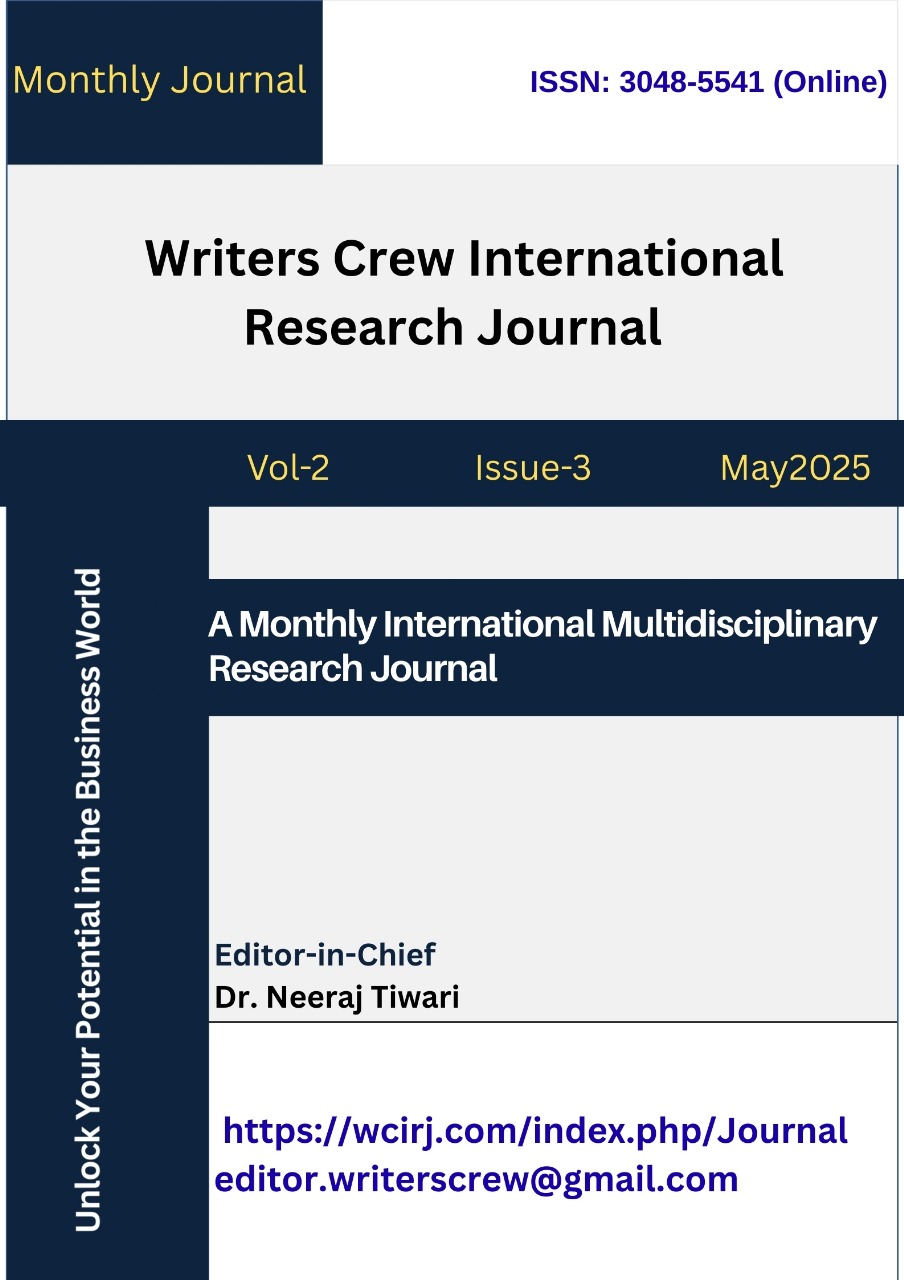
Role of Parental Involvement in Children's Academic Achievement
Vol. 2 No. Issue: 3, May, pg. 1345-1376 (2025) (2025)AbstractParental involvement plays a vital role in shaping children’s academic achievement. Parents serve as the first educators and continue to influence a child’s learning trajectory through active engagement in school activities, support with homework, motivation, and the creation of a conducive learning environment at home. This research paper explores the multifaceted role of parental involvement in the educational success of children, analyzing different dimensions including emotional, social, and academic aspects. The study reviews existing literature, presents empirical findings, and discusses the implications of parental involvement across socioeconomic, cultural, and educational contexts.
Keywords
The abstract emphasizes how parental involvement enhances student motivation, attendance, self-esteem, and long-term academic outcomes. It highlights the challenges parents face due to economic hardship, lack of educational background, or limited time, and explores strategies to bridge these gaps. The research methodology relies on surveys and analysis of responses from parents, teachers, and students across selected schools. Through data interpretation and comparative analysis, the study identifies strong positive correlations between parental support and children’s academic success. The conclusion reiterates that parental involvement is a significant determinant of academic achievement, calling for school policies and community initiatives to strengthen parent-school partnerships.
Ultimately, the study provides actionable insights for educators, policymakers, and parents themselves to foster an environment where children can thrive academically. The findings not only confirm the existing scholarly consensus but also contribute to context-specific understanding in the surveyed population.Parental Involvement, Academic Achievement, Student Motivation, Parent-School Partnership, Educational Success
-
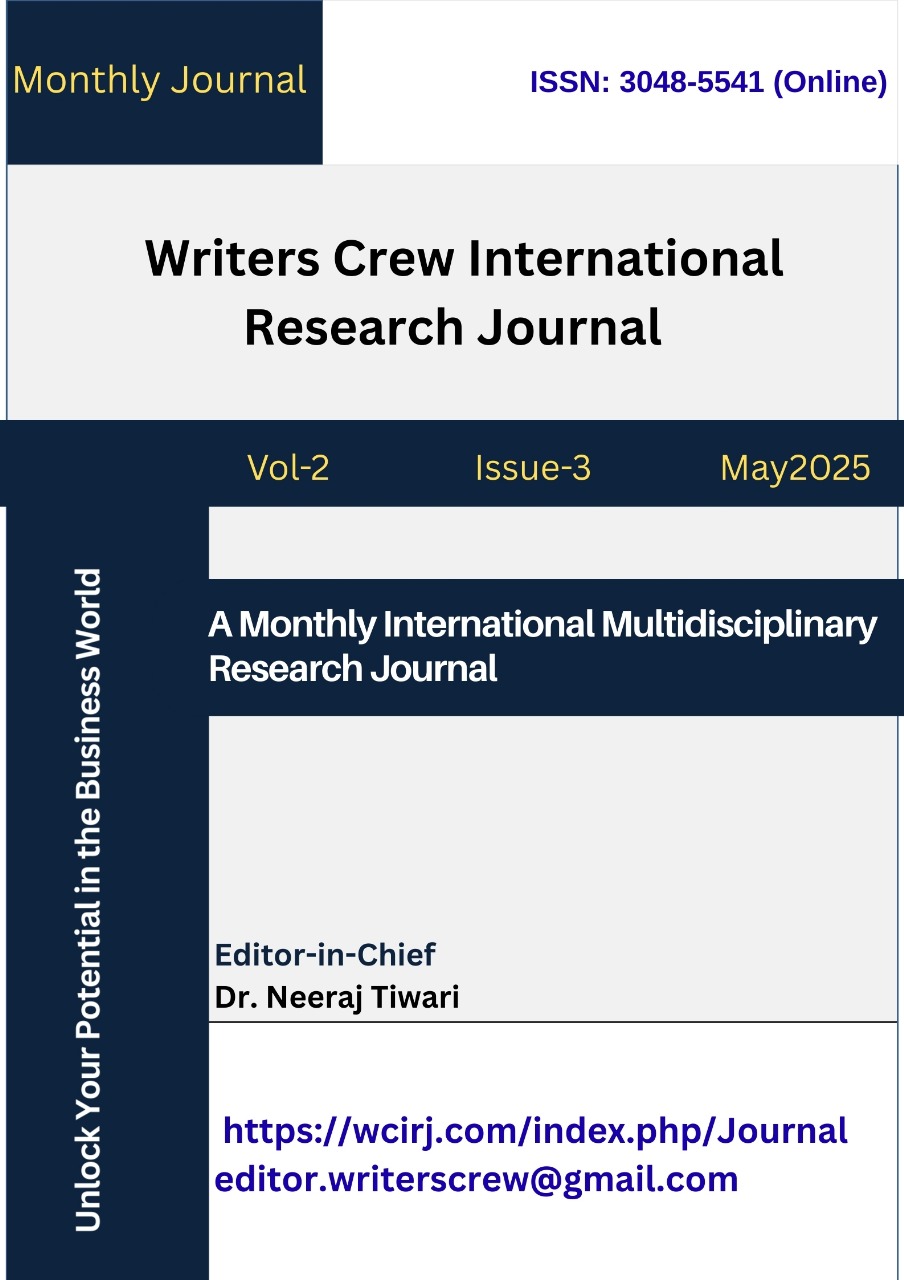
योगाभ्यास द्वारा विद्यालयी विद्यार्थियों में आत्मानुशासन और मानसिक संतुलन का विकास
Vol. 2 No. Issue: 3, May, pg. 1287-1314 (20 (2025)सारांश
यह शोध पत्र वद्यालयी वद्या थयों में योगाभ्यास के माध्यम से आत्मानुशासन और मान सक संतुलन
के वकास का वश्लेषण करता है। वतमान समय में वद्या थयों को अनेक शै क्षक, सामािजक और
मान सक चुनौ तयों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौ तयों का सामना करने के लए आवश्यक है क
उनके अंदर आत्मानुशासन और मान सक िस्थरता का वकास हो। योगाभ्यास, जो प्राचीन भारतीय
परंपरा का एक अ भन्न अंग है, इन दोनों गुणों के वकास में प्रभावी सद्ध हो सकता है।
यह अध्ययन वशेष रूप से यह देखने का प्रयास करता है क नय मत योग अभ्यास से वद्या थयों में
आत्मानुशासन कैसे वक सत होता है और वे अपने मान सक और शारी रक स्वास्थ्य को कैसे सुदृढ़ कर
सकते हैं। अध्ययन में वद्यालय स्तर पर व भन्न आयु वग के वद्या थयों पर योग के प्रभाव का
परीक्षण कया गया है। अध्ययन के दौरान, योग के अभ्यास से वद्या थयों में स्व-अनुशासन, धैय,
आत्म- नयंत्रण, मान सक िस्थरता, तनाव एवं चंता में कमी, ध्यान कें त करने की क्षमता, और
सकारात्मक मान सकता जैसे लक्षणों में सुधार पाया गया है।
इसके अत रक्त, यह शोध शक्षकों और अ भभावकों के लए भी मागदशन प्रदान करता है क कैसे योग
को शै क्षक कायक्रमों में शा मल करके वद्या थयों के शारी रक एवं मान सक वकास को प्रोत्सा हत
कया जा सकता है। इस अध्ययन के नष्कष यह स्पष्ट करते हैं क योगाभ्यास न केवल वद्या थयों के
शारी रक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बिल्क उनके व्यिक्तत्व का समग्र वकास भी करता है, िजससे वे
जीवन में अ धक अनुशा सत, आत्म वश्वासी और मान सक रूप से िस्थर बनते हैं।
मूल शब्द- योगाभ्यास, आत्मानुशासन, मान सक संतुलन, वद्यालयी वद्याथ, मान सक स्वास्थ्य -
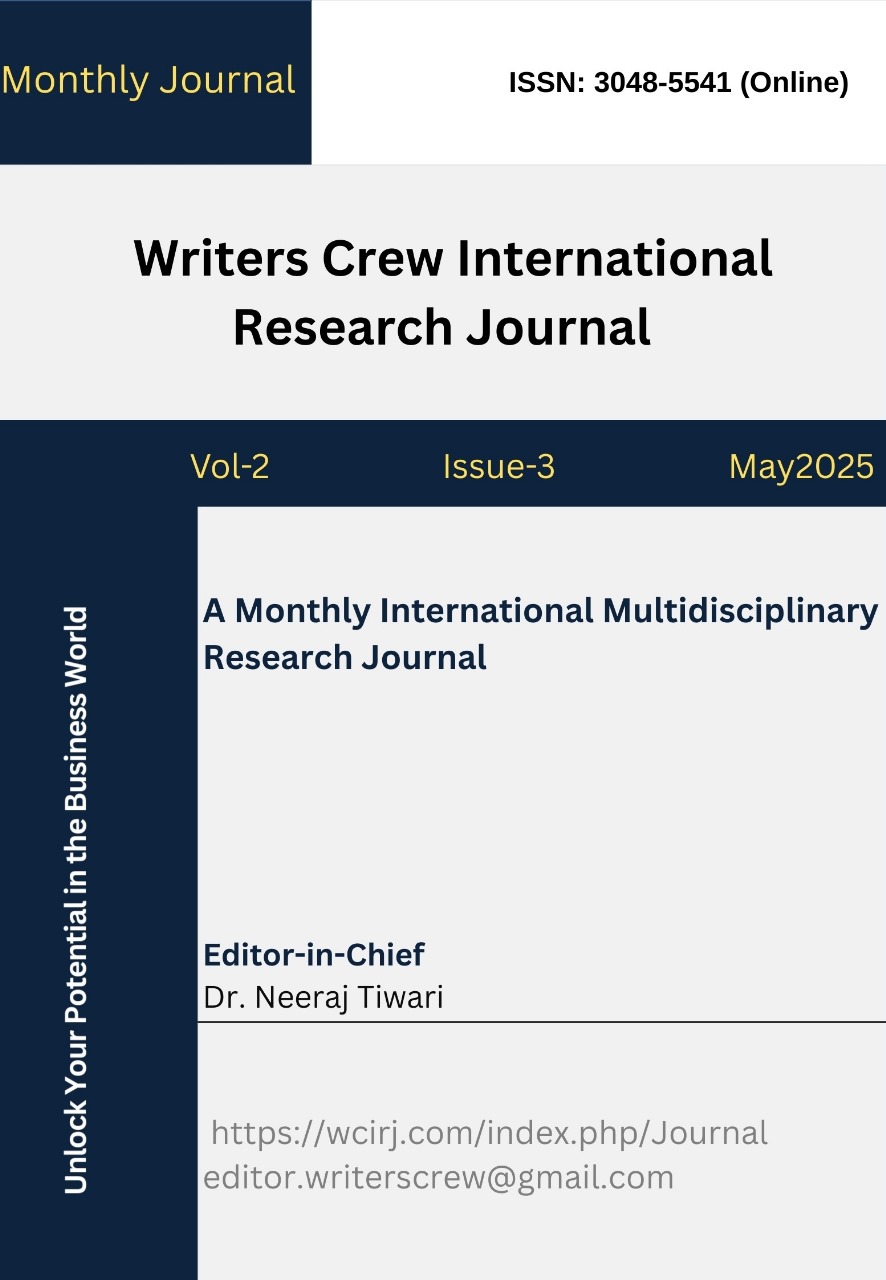
शिक्षा में भगवदगीता की प्रासंगिकता का अध्ययन
Vol. 2 No. Issue: 3, May , pg. 1273-1286 (2025)सार
भगवद्गीता की प्रमुख विशेषता है, उसकी व्यवहारिकता और प्रासंगिकता, जो समाज के व्यवहार में प्रचलित हो न कि सिद्धान्तों मात्र की हो। भगवद्गीता में मात्र तत्त्व ज्ञान ही नहीं वरन् व्यवहारिक दर्शन सर्वथा दर्शनीय है। भगवद्गीता दार्शनिक विवेचन ही नहीं है वरन् भगवद्गीता मानव को केन्द्र में रखकर मानव के सर्वतोन्मुखी कल्याण के उपायों को भी प्रस्तुत करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाना हो गया है जबकि भगवद्गीता पाठ्यवस्तु को छात्रों के मानसिक स्तरानुसार उसकी योग्यता, अभिरूचि आदि के अनुसार व्यवहार में उसके प्रयोग करती है।
शब्द कुंजीः शिक्षा, भगवद्गीता, प्रासंगिकता, दर्शन, नीतिशास्त्र, अभिरूचि ।
-
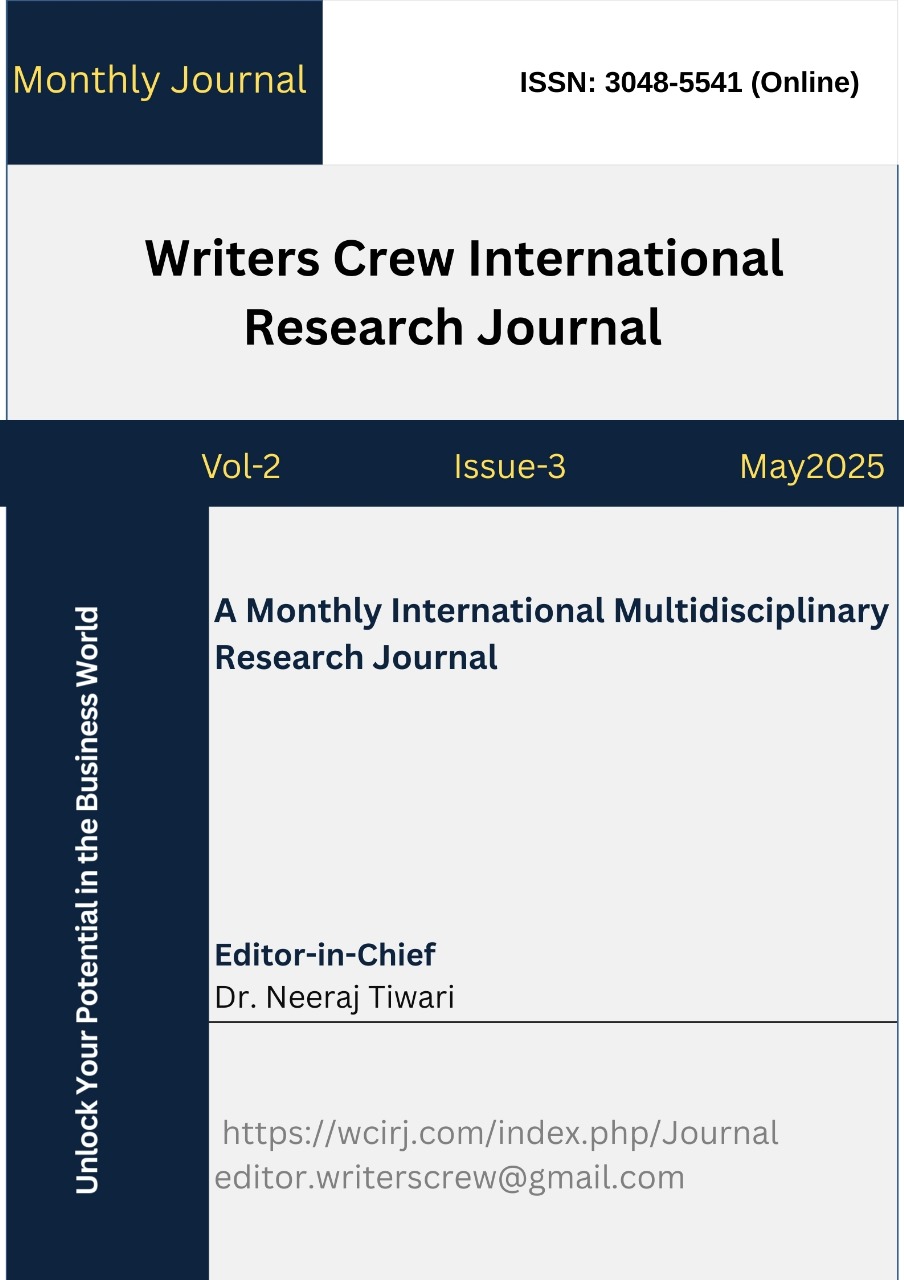
उत्तराखंड की महिला उद्यमिता: अवसर समस्याएं और संभावनाएं
Vol. 2 No. Issue: 3, May, pg. 1225-1272 (2025)सार
यह शोध पत्र उत्तराखंड राज्य में महि ला उद्यमि ता के वि भि न्न पहलुओं का वि श्लेषण करता है, जि समें उपलब्ध अवसरों, सामना की जाने वाली समस्याओं और भवि ष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रि त कि या गया है। उत्तराखंड की वि शि ष्ट सामाजि क-आर्थि र्थिक और भौगोलि क परि स्थि ति यां महि ला उद्यमि यों के लि ए अद्वि तीय चुनौति यां और अवसर प्रस्तुत करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन कारकों की गहन जांच करना है ताकि महि ला उद्यमि ता को बढ़ ावा देने के लि ए प्रभावी रणनीति यों का वि कास कि या जा सके।
शोध एक मि श्रि त दृष्टि कोण अपनाता है, जि समें प्राथमि क डेटा संग्रह के लि ए सर्वे र्वेक्षणों और साक्षात्कारों का उपयोग कि या गया है, साथ ही द्वि तीयक डेटा के रूप में सरकारी रि पोर्टों और प्रासंगि क साहि त्य की समीक्षा भी की गई है। अध्ययन उत्तराखंड के वि भि न्न क्षेत्रों की महि ला उद्यमि यों से जानकारी एकत्र करता है ताकि उनकी अनुभवों और दृष्टि कोणों का व्यापक चि त्र प्राप्त कि या जा सके।
प्रारंभि क नि ष्कर्ष र्ष बताते हैं कि उत्तराखंड में कृषि , हस्तशि ल्प, पर्य र्यटन और सेवा क्षेत्र में महि ला उद्यमि यों के लि ए महत्वपूर्ण र्ण अवसर मौजूद हैं। हालांकि , उन्हें वि त्तीय संसाधनों तक पहुंच की कमी, वि पणन चुनौति यों, सामाजि क और सांस्कृति क बाधाओं, और कौशल वि कास की आवश्यकता जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ ता है। इन समस्याओं के बावजूद, महि ला उद्यमि यों में दृढ़ ता और नवाचार की भावना स्पष्ट है, जो भवि ष्य के लि ए सकारात्मक संभावनाएं दर्शा ती है।
यह शोध पत्र नीति नि र्मा ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हि तधारकों के लि ए मूल्यवान अंतर्दृ ष्टि प्रदान करता है जो उत्तराखंड में महि ला उद्यमि ता को समर्थ र्थन और बढ़ ावा देने के लि ए प्रयासरत हैं। नि ष्कर्षों के आधार पर, वि त्तीय सहायता, कौशल वि कास कार्य र्यक्रम, वि पणन सहायता और अनुकूल नीति गत माहौल बनाने के लि ए वि शि ष्ट सुझाव प्रस्तुत कि ए गए हैं। इस शोध के माध्यम से उत्तराखंड में महि ला उद्यमि यों के सशक्ति करण और राज्य के समग्र आर्थि र्थिक वि कास में उनके योगदान को बढ़ ाने की दि शा में महत्वपूर्ण र्ण कदम उठाए जा सकते हैं।
मुख्य शब्द: महि ला उद्यमि ता, उत्तराखंड, अवसर, समस्याएं, संभावनाएं, ग्रामीण वि कास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, नीति । -
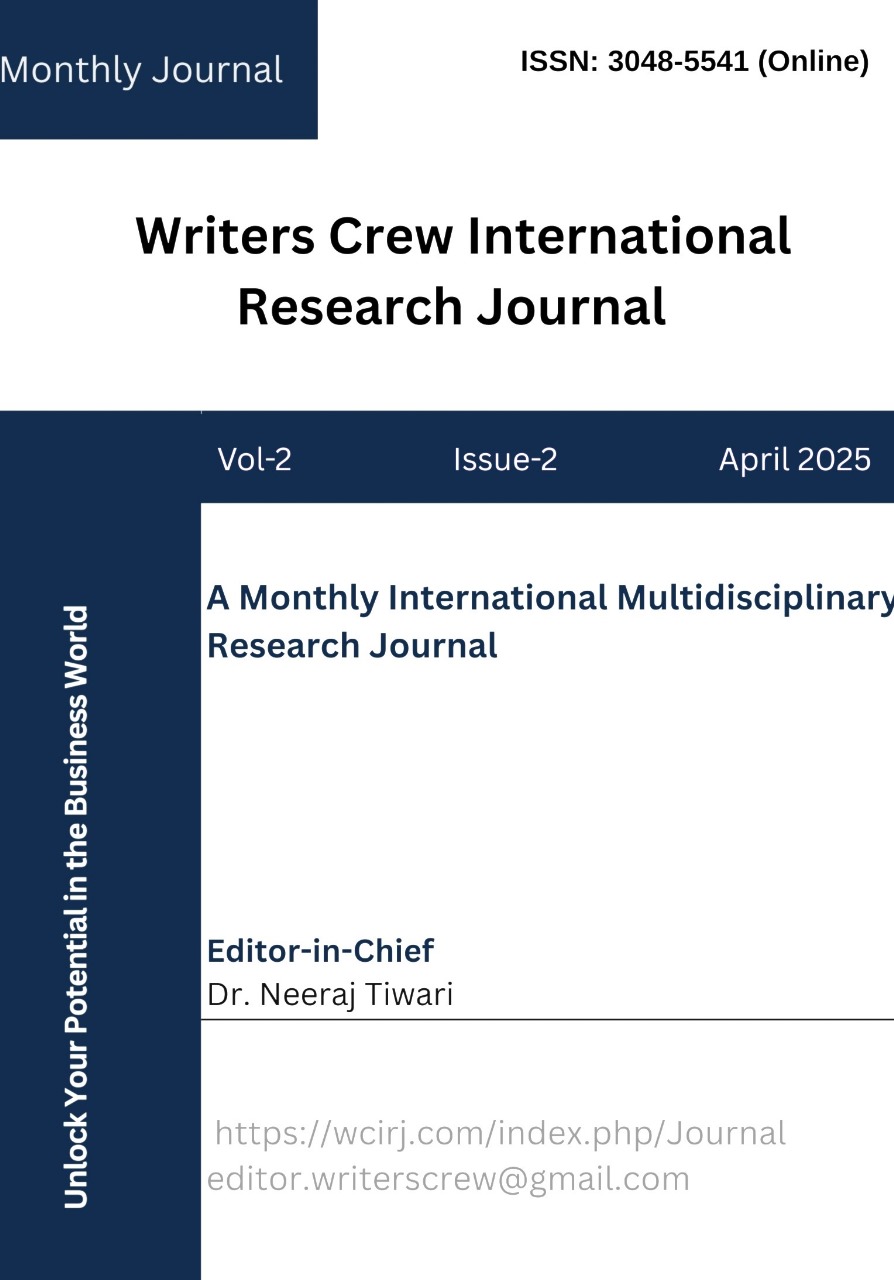
Applications of Nanotechnology in Drug Delivery Systems
Vol. 2 No. Issue: 2, April, 1166-1179 (2025)ABSTRACT: In the recent past, the targeted drug delivery has gained more attention for various advantages. Amongst the plethora of Avenues explored for targeted drug delivery. Nanoparticles are particulate dispersions or solid particles with a size in the range of 10-1000nm. The drug is dissolved, entrapped, encapsulated or attached to a nanoparticle matrix. Depending upon the method of preparation, nanoparticles, nanospheres or nanocapsules can be obtained. The major goals in designing nanoparticles as a delivery system are to control particle size, surface properties and release of pharmacologically active agents in order to achieve the site- specific action of the drug at the therapeutically optimal rate and dose regimen. Present review reveals the methods of preparation, characterization and application of several nanoparticulate drug delivery systems.
KEYWORDS: Nano particle drug delivery system, nanospheres, nanocapsules. -
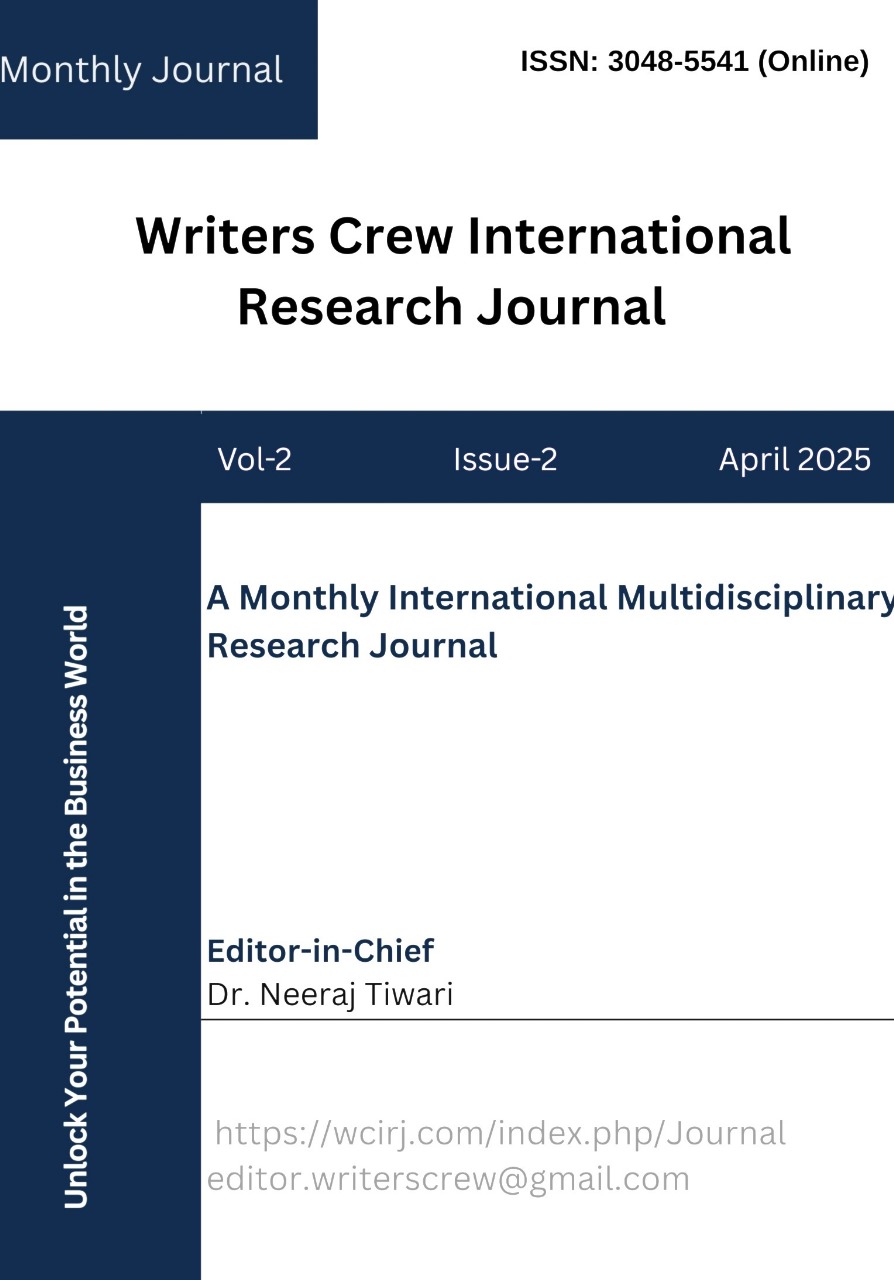
Challenges and Research on Quality Education in India
Vol. 2 No. Issue: 2, April, pg. 1213-1224 (2025)ABSTRACT
An effort has been made through this seminar paper to have an idea of the challenges
that are being faced in modern times while providing quality education and the current
research that is going on this topic. The paper gives an overview of the quality
education as UNICEF’s sustainable development goal number four. It tries to answer
some specific questions as to why quality education. How to ensure quality education?
What are the challenges of implementing quality education? How proper assessment,
monitoring, governance, and accountability can help to develop quality education? Can
spirituality and morality be of any help in this field? Or the modern technologies like ICT
and Artificial Intelligence can assist in this regard? What is the situation of quality
education in India? In the end, there will be an attempt to have some suggestions
regarding the proper implementation of quality education.
Keywords: Quality Education, Challenges, Solutions, Research, Indian Perspective -
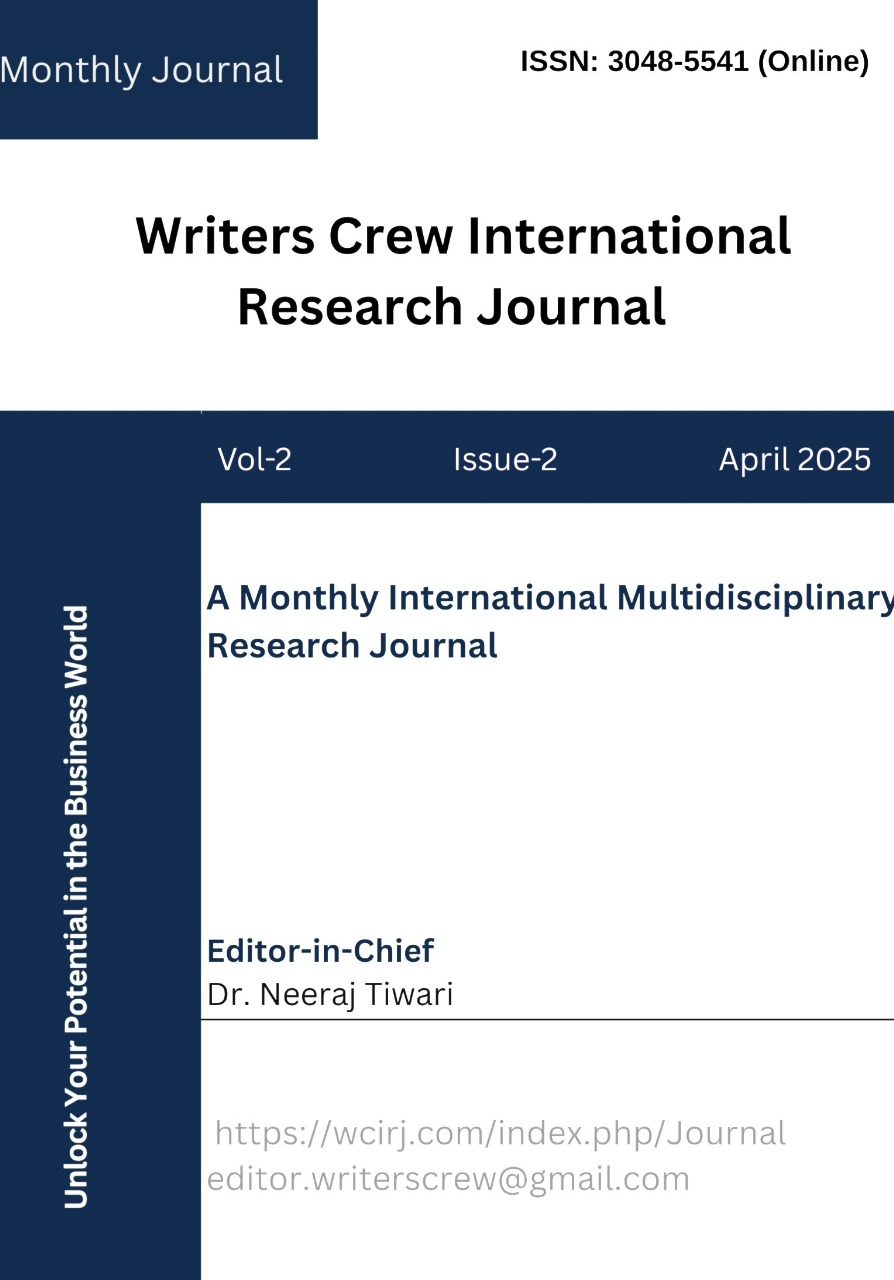
आर्थिक समृद्धि बनाम ग्रामीण वित्तीय समावेशन
Vol. 2 No. Issue: 2, April, pg. 1180-1212 (2025)सारांश
वि
त्तीय समावेशन" और "समावेशी वि कास" आज प्रचलि त शब्द हैं। समावेशी वि कास कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाता है। यह, बदले में, कई कारकों पर नि र्भ र्भर करता है - सबसे महत्वपूर्ण र्ण है "वि त्तीय समावेशन", जो समावेशी वि कास को बढ़ ावा देने में रणनीति क भूमि का नि भाता है और कमजोर वर्गों को वि त्त के नि यमि त और वि श्वसनीय स्रोत प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद करता है। इस दि शा में, भारत सरकार ने वि त्तीय समावेशन के अपने अभि यान में बैंक रहि त परि वारों तक औपचारि क वि त्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ ाने और उनका लाभ उठाने के लि ए कई उपाय कि ए हैं। इस पेपर का उद्देश्य वि त्तीय समावेशन की प्रकृति और सीमा और समावेशी वि कास पर ध्यान केंद्रि त करते हुए कमजोर वर्गों से संबंधि त परि वारों की सामाजि क आर्थि र्थिक स्थि ति पर इसके प्रभाव का आकलन करना है। इसका वि श्लेषण वि त्तीय पहुंच और आर्थि र्थिक वि कास पर सैद्धांति क पृष्ठभूमि और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जि ले से एकत्र प्राथमि क आंकड़ ों का वि श्लेषण करके कि या गया है। नतीजे बताते हैं कि वि त्तीय समावेशन की प्रकृति और सीमा में असमानता है।
औपचारि क बैंकि ंग सेवाओं तक पहुंच और उनका लाभ उठाने से कमजोर वर्गों के परि वारों की सामाजि क-आर्थि र्थिक स्थि ति में सकारात्मक बदलाव का मार्ग र्ग प्रशस्त होता है, जो सहसंबद्ध होते हैं, जि ससे समावेशी वि कास होता है, जि सके आधार पर पेपर वि त्तीय प्रणाली को और अधि क समावेशी बनाने के लि ए एक मॉडल का प्रस्ताव करता है।
सामाजि क आर्थि र्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 महत्वपूर्ण र्ण आर्थि र्थिक रुझानों को उजागर करने वाली एक उल्लेखनीय रि पोर्ट र्ट हैI ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामि त्व, रोजगार, स्कूली शि क्षा के औसत वर्ष र्ष (एमवाईएस) और सामाजि क समावेशन के मामले में। स्थानि क आकस्मि क श्रम, गरीबी, कि सान कार्ड र्ड के माध्यम से कम पहुंच, वि त्तीय के चि ंताजनक नि ष्कर्षों को देखते हुए पि रामि ड के नि चले भाग के
लोगों के लि ए समावेशन गंभीर नीति गत चुनौति याँ पैदा करता है। अखबार का तर्क र्क है कि अधि कार आधारि त दृष्टि कोण जो अवसर, सशक्ति करण और सामाजि क सुरक्षा को प्राथमि कता देता है, सही होगा आगे बढ़ ने का रास्ता। नीति प्रभावशीलता सूचकांक (पीईआई) दृष्टि कोण हमारे असंतोषजनक कानून के लि ए उपयोगी अंतर्दृ ष्टि प्रदान करता है और व्यवस्था की स्थि ति और खराब रोजगार के अवसर। यह ग्रामीण शहरी प्रवासन से बचने की वकालत करता है रणनीति ; इसके बजाय यह कृषि (आर एंड डी), कृषि उद्योग वि कास, गुणवत्तापूर्ण र्ण शि क्षा आदि में नि वेश का आह्वान करता है वि कास और मानव वि कास सूचकांक (एचडीआई) को एकजुट करने के लि ए कौशल प्रशि क्षण।
यह पेपर इसकी पहचान से नि पटने का प्रयास करता हैl सेवा केंद्र और स्थानि क व्यवस्था की गणना जौनपुर जि ले में सेवा केन्द्रों का पूरक क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जौनपुर जि ला I अध्ययन क्षेत्र स्थि त है मध्य गंगा मैदान का पूर्वी उत्तर प्रदेश। अध्ययन है वि शेष रूप से ब्लॉक स्तर पर एकत्र कि ए गए द्वि तीयक डेटा पर आधारि त वि भि न्न कार्या लयों सl केंद्रीयता स्कोर की गणना की गई है कार्या त्मक केंद्रीयता जैसे तीन प्रकार के सूचकांकों के आधार पर सूचकांक, कार्य र्यशील जनसंख्या सूचकांक और तृतीयक जनसंख्या सूचकांक।
पाँच में से न्यायि क रूप से चुने गए 31 कार्य र्य या सेवाएँ हैं क्षेत्र (प्रशासनि क, कृषि और वि त्तीय, शैक्षि क, स्वास्थ्य और परि वहन और संचार) को मापने के लि ए सेवा केंद्र की केंद्रीयता. थीसेन बहुभुज और बेरी मापने के लि ए ब्रेकि ंग पॉइंट वि धि का उपयोग कि या गया है पूरक क्षेत्र l कुल 88 सेवा केन्द्र बनाये गये हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें क्रम की सेवा के रूप में पहचान की गई केंद्र।
कीवर्ड र्ड: वि त्तीय समावेशन, वि त्तीय समावेशन का प्रभाव, सामाजि क-आर्थि र्थिक स्थि ति , समावेशी वि कास Vol. 2, Issue: 2, April, -
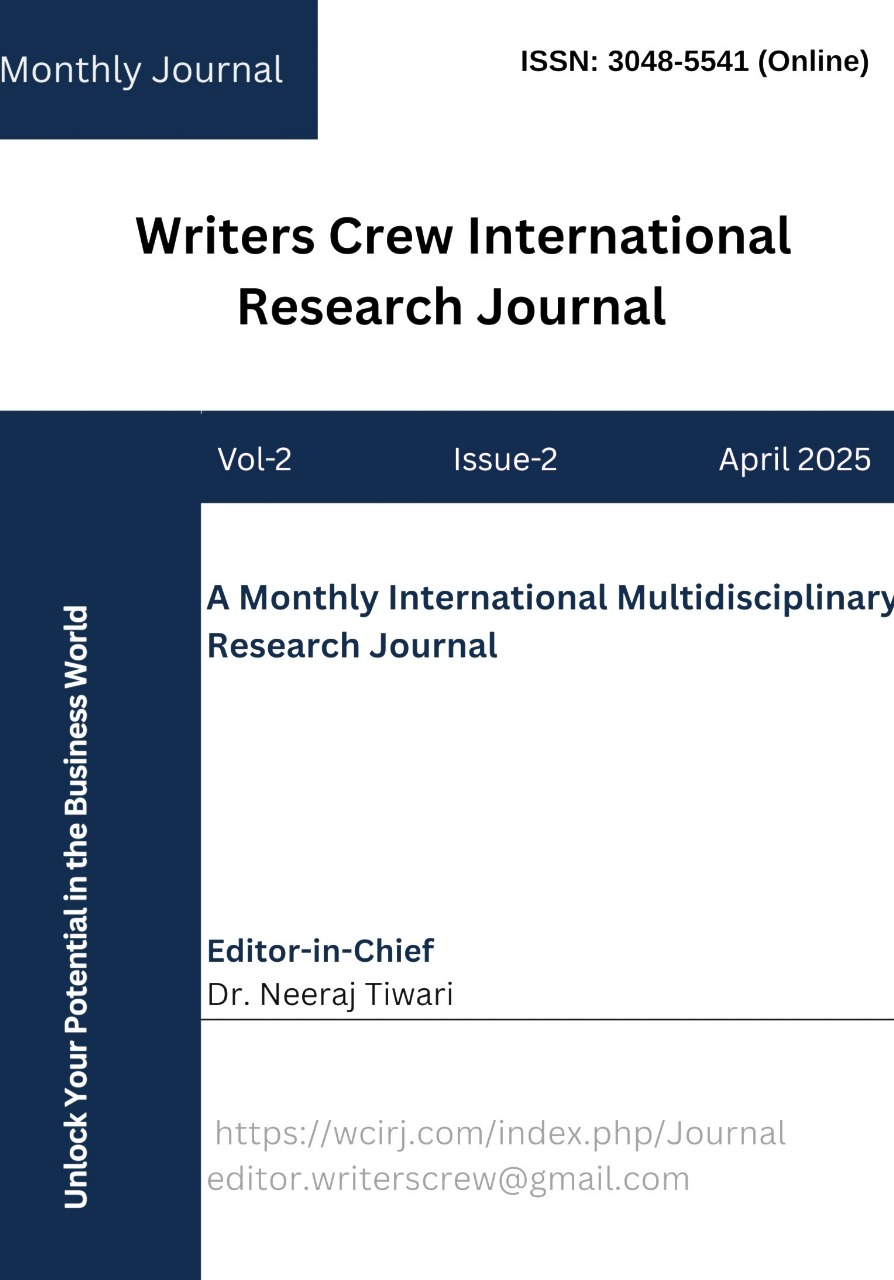
हिमालय क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका: एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन
Vol. 2 No. Issue: 2, April , pg. 1129-1165 (2025)सार
यह शोध पत्र हि मालय क्षेत्र में महि लाओं की बहुआयामी भूमि का का एक सामाजि क-आर्थि र्थिक वि श्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन इस दुर्ग र्गम और पारि स्थि ति क रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महि लाओं द्वारा नि भाई जाने वाली महत्वपूर्ण र्ण भूमि काओं का पता लगाता है, जि समें घरेलू कार्यों , कृषि , वन संसाधनों के प्रबंधन, आजीवि का सृजन और सामुदायि क वि कास में उनका योगदान शामि ल है।
अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे महि लाएं पारंपरि क रूप से इस क्षेत्र की अर्थ र्थव्यवस्था और सामाजि क संरचना की रीढ़ रही हैं, अक्सर सीमि त संसाधनों और चुनौतीपूर्ण र्ण परि स्थि ति यों के बावजूद महत्वपूर्ण र्ण जि म्मेदारि यों को नि भाती हैं। यह उनके श्रम शक्ति में भागीदारी, नि र्ण र्णय लेने की प्रक्रि याओं में उनकी भूमि का, और स्थानीय अर्थ र्थव्यवस्थाओं पर उनके प्रभाव का वि श्लेषण करता है।
इसके अति रि क्त, यह शोध पत्र उन सामाजि क-आर्थि र्थिक चुनौति यों और बाधाओं का भी परीक्षण करता है जि नका सामना हि मालयी क्षेत्रों की महि लाओं को करना पड़ ता है, जैसे कि शि क्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमि त पहुंच, भूमि अधि कारों की कमी, लैंगि क असमानता, और जलवायु परि वर्त र्तन और प्राकृति क आपदाओं का बढ़ ता प्रभाव।
प्राथमि क और माध्यमि क डेटा के संयोजन का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन हि मालय क्षेत्र में महि लाओं की सशक्ति करण के लि ए आवश्यक नीति यों और हस्तक्षेपों के लि ए सि फारि शें प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नीति नि र्मा ताओं, वि कास एजेंसि यों और शोधकर्ता ओं को इस क्षेत्र में लैंगि क समानता -
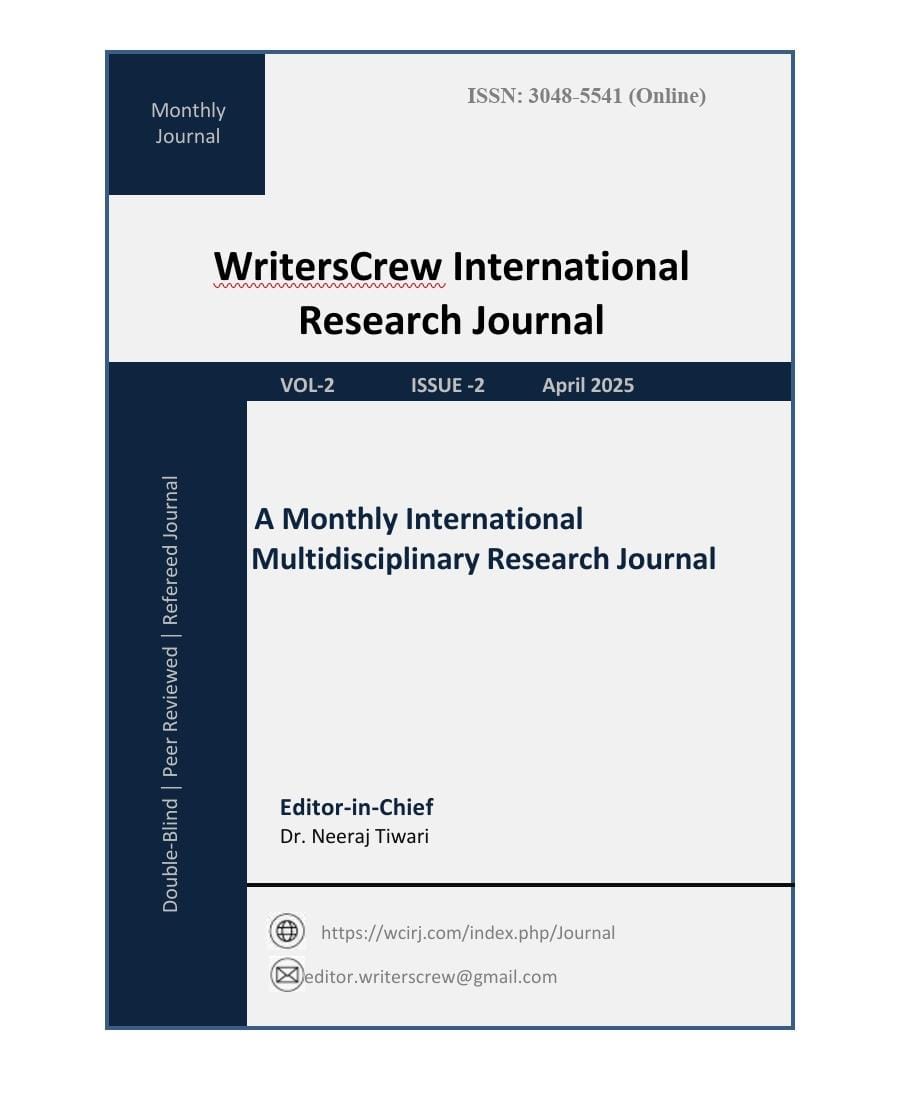
माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन
Vol. 2 No. Issue: 2, April , pg. 1121-1128 (2025)सार
माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत् छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन हैं। इस अध्ययन में छात्र और छात्राओं के पारिवारिक वातावरण के शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। जनसंख्या के रूप में मेरठ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को जनसंख्या माना गया है। माध्यमिक स्तरीय स्कूलों का चयन उद्देश्यपरक विधि से किया गया है शोध हेतु 150 छात्र एवं 150 छात्राओं अर्थात् कुल 300 छात्रों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि से किया गया है। उपकरण के रूप में मिश्रा के०एस० द्वारा निर्मित 'पारिवारिक वातावरण अनुसूची एवं छात्रों के कक्षा 9 की परीक्षा में प्राप्त अंकों को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में रखा गया है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए टी-अनुपात एवं सहसम्बन्ध गुणांक सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत् छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण पर प्रभाव है अर्थात् छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है।
बीज शब्द- माध्यमिक स्तरीय स्कूल, छात्र, शैक्षिक उपलब्धि, पारिवारिक वातावरण।
-

माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षक योग्यता के प्रभाव का अध्ययन
Vol. 2 No. Issue: 1, March, pg. 1112-1120 (2025)सार
माध्यमिक स्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत् छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षक योग्यता के प्रभाव का अध्ययन है। प्रस्तुत शोध पत्र में छात्र-छात्राओं की उपलब्धि को शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के साथ अध्ययन किया गया है। शोध की सर्वेक्षण एवं विश्लेषण विधि द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययन में जनपद मेरठ के 06 माध्यमिक स्तरीय स्कूलों से 30 छात्र एवं 30 छात्राओं को यादृच्छिक विधि से चयन किया गया है। निष्कर्ष रूप से शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से अधिक उसके शिक्षण की कला, उसका व्यवहार, अंतर्वस्तु का ज्ञान एवं ज्ञान को स्थानान्तरण करने की कला महत्त्वपूर्ण है।
बीज शब्द- माध्यमिक स्तरीय स्कूल, शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक योग्यता।
-
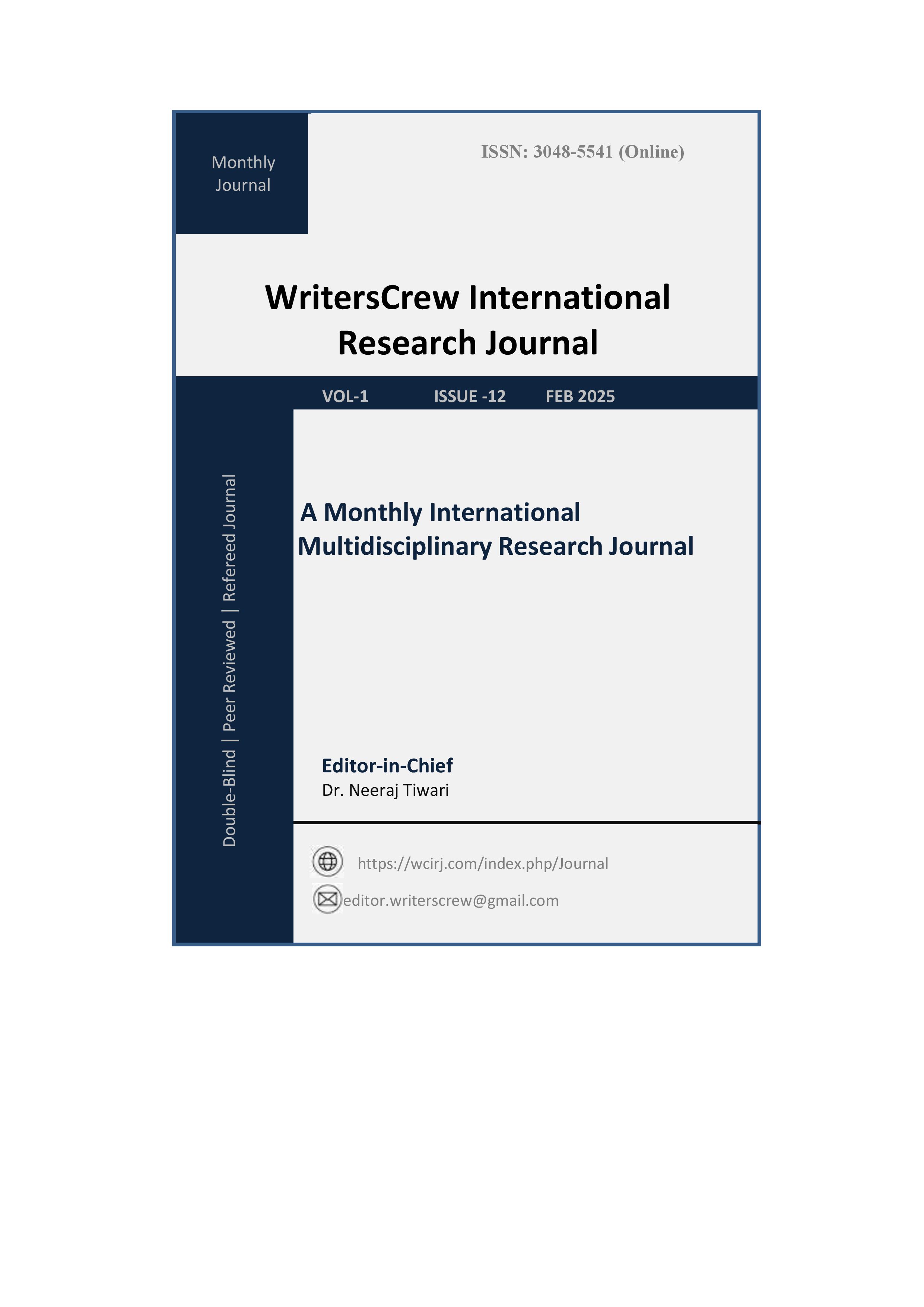
Impact of Urbanization on Traditional Rural Communities
Vol. 2 No. Issue 1March, 1100-1111 (2025)Abstract: Though with slight ups and downs, Vietnamese economies have been flourishing for recent
decades. Just like other remaining historical districts in Asia, those of Vietnam have been going through
rapid urbanization and transformation. The rapid urbanization impacts on traditional living environment.
This paper examines the impacts of rapid urbanization to traditional living environment and community
linkage, illustrating a case study of the Gia Hoi area of the historic old district in the city of Hue in
Central Vietnam. To identify the impacts, a comparative analysis is conducted between neighbors along
a main street which were more impacted by urbanization and those along a small alley which were less
impacted. Through the analysis of field and questionnaire surveys, it found out that socioeconomic
conditions, in particular, community linkage of households along main street and small ally varied
significantly. It argues that in historical district, social capital is not well-spread, but rather concentrated
along small allies, and small allies play an important role for sustainable community.
Key words: Community linkage, impact of urbanization, traditional living environment, historical city. -
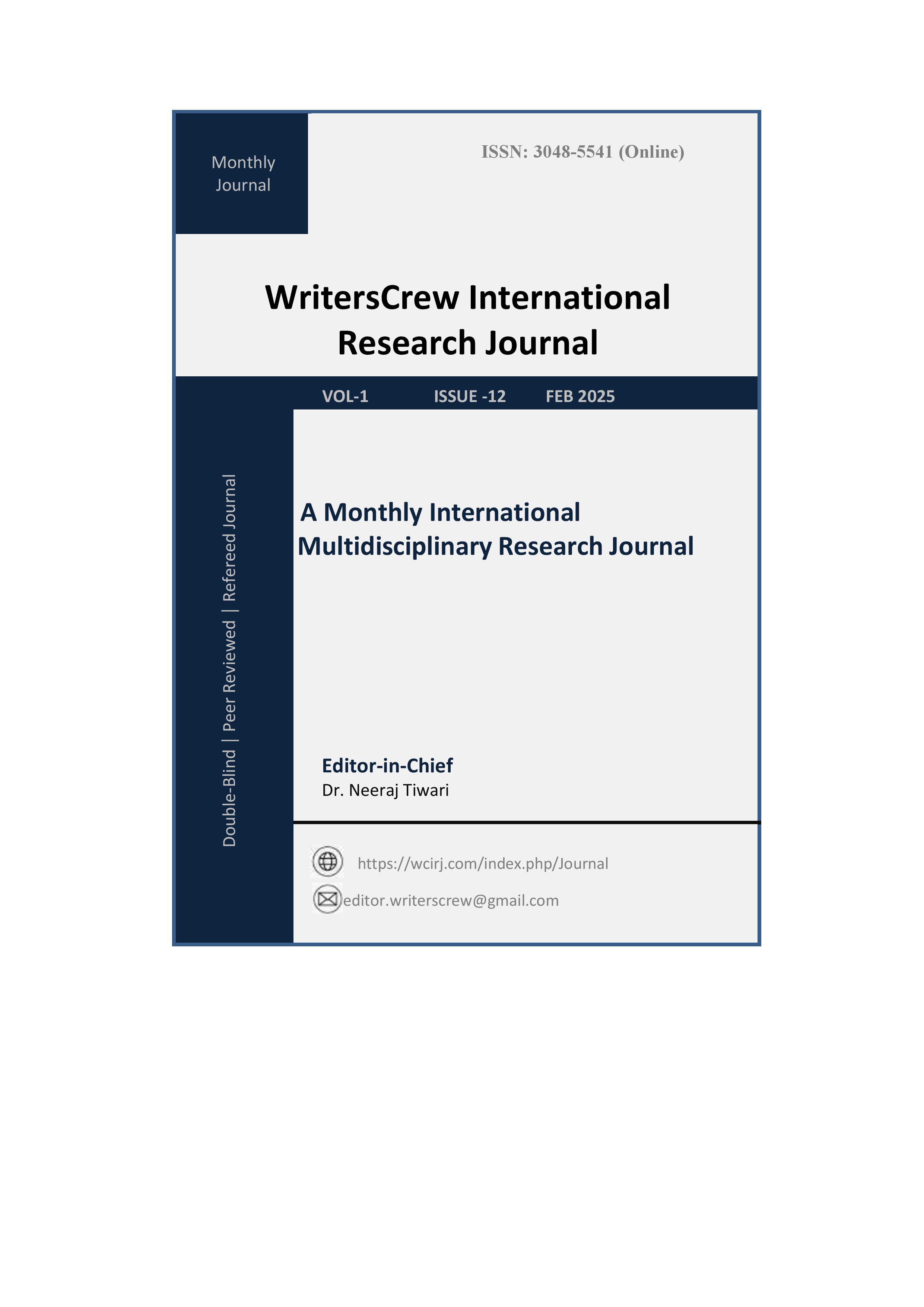
Teacher Burnout: Causes, Impacts, and Mitigation Strategies
Vol. 2 No. Issue 1March, 1089-1099 (2025)Abstract - As we know burnout is a highly growing problem across the world whether in
the students, teachers, parents, doctors, or all the fields. And teacher burnout is one of the
most rapidly growing in society. Teachers' burnout impacts on their psychological health
which affects their performance in the job, the ability of providing the good quality
education they provide to their students and also impact their relationships with their
students and colleagues due to emotional exhaustion. This review paper collects data by
gathering information from 2000 to 2025 studies, which are especially focused on recent
years or we may say after covid 19 health crises. This review paper describes what is the
meaning of teachers burnout, what are the causes of teachers burnout, how it impacts
their teaching and their relations with students. It also focuses on the situation of teachers
after publishing National Education Policy (NEP) 2020 in India. This paper wishes to
provide help to policy makers, school management and leaders or educators for making
better understanding about teacher burnout and taking strict steps towards reducing it and
providing mental health. -

A Comparative Analysis of Educational Curriculum Systems: Perspectives on Structure, Content, and Pedagogical Approaches
Vol. 2 No. Issue: 1, March, 1069-1088 (2025)ABSTRACT: China is famous for its very high-quality education; it has a very detailed and
structured education system, from primary to university. China also has a culture that values
education, so its people care and try hard to improve the quality of education. This research
aims to compare curriculum systems in Indonesia and China. This research method is a
literature review carried out by collecting relevant sources and using a descriptive analysis
approach. The results of this research are: 1) Both Indonesia and China have carried out
curriculum reforms to follow society's needs. 2) Indonesia has a 12-year compulsory education
program, while China has nine years. 3) Despite their differences, national education goals in
both countries are the same: to develop balanced, qualified, and characterized individuals to
contribute to national development. 4) The government determines the content/material taught
in both countries at the elementary-middle school level. However, China does not have
mandatory subjects at the high school level, while the government still determines Indonesia. 5)
Learning strategies in Indonesia include group, project, and inquiry-based learning; China has
unique strategies, such as implementing naps during learning. 6) National exams are no longer
implemented in Indonesia, while there is still a national exam known as the Gaokao Exam in
China.
KEYWORDS: Curriculum, China, Indonesia, Education -

ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN DEVELOPING UNDERGRADUATE STUDENTS' BEHAVIOUR
Vol. 2 No. Issue: 1, March , pg. 1044-1068 (2025)Abstract
The present research paper has been conducted on the topic of environmental education and the
undergraduate student behaviours across the globe. The aim of the research paper is to analyse the
role of environmental education along with its impact on developing undergraduate students’
behaviour. Therefore, the researcher has applied the Social Learning Theory and Ecological
Systems Theory in the literature review section for providing an in-depth understanding of the
learning and behavioural aspects of the undergraduate students regarding the emergence of
environmental education. However, the researcher has integrated many appropriate research
methodologies in this research for offering a suitable and acceptable conclusion on this research
topic. However, the thematic analysis has found out that the consideration of environmental
education in the undergraduate courses can allow the students to improve their awareness regarding
sustainability and environmental issues in the surroundings. Despite the issues of this curriculum,
the researcher has stated that the teachers and the education ministry of the countries can promote
the environmental themes across the curriculum, utilize the technology, promote practical learning
as well as foster a sense of environmental responsibility.
Keywords
Environmental Education (EE), environmental knowledge, responsibility towards environment,
sustainable practices, climate change, undergraduate students’ behaviour, Social Learning Theory
and Ecological Systems Theory -
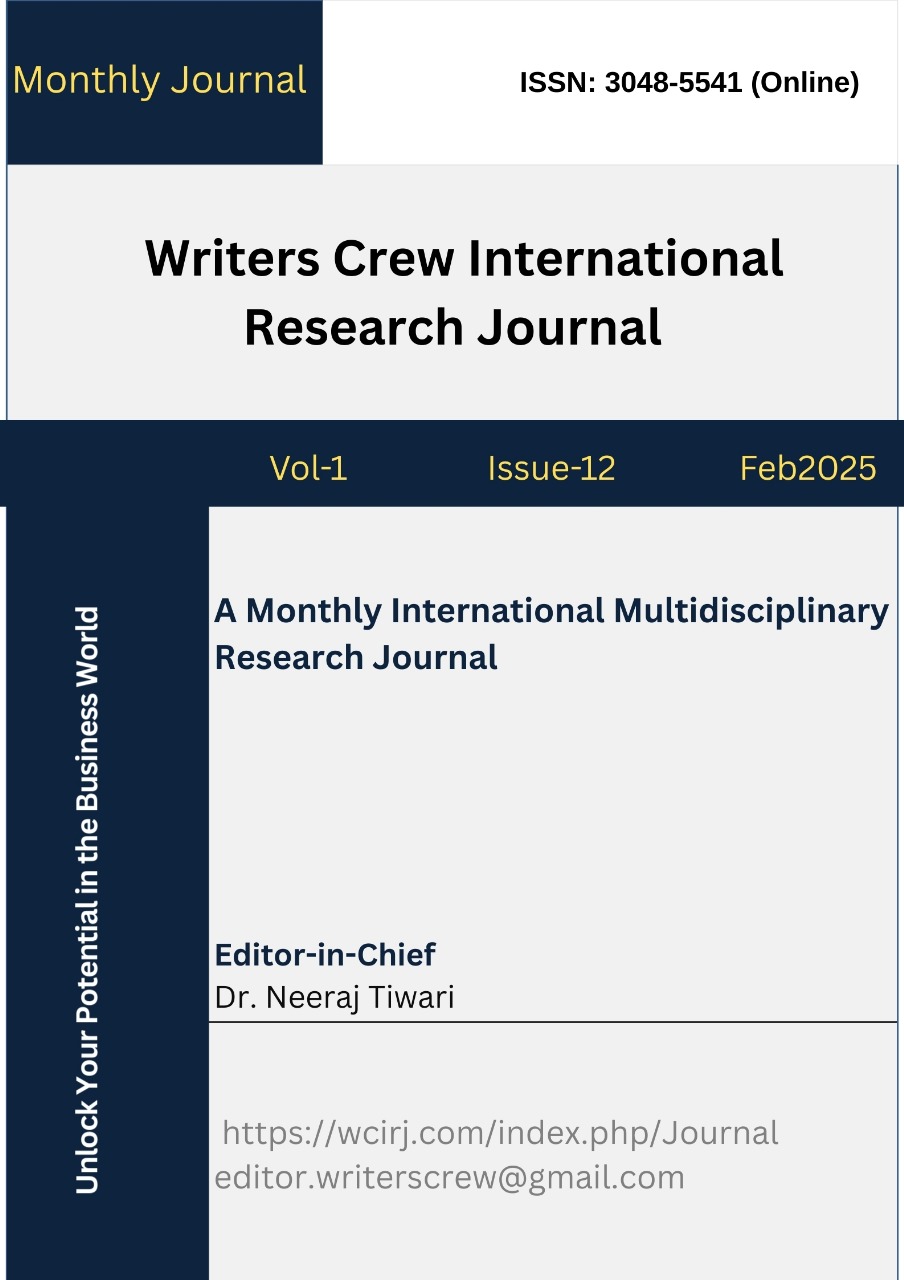
PARENTAL PERCEPTION AND SUPPORT FOR VOCATIONAL EDUCATION AT THE HIGHER SECONDARY LEVEL
Vol. 1 No. Issue: 12, February , pg. 1019-1043 (2025)Abstract
This research has explored how the perception of parents has shaped choices of students to
pursue vocational education and training (VET) at the higher secondary level. Many parents
worldwide have preferred traditional college degrees over VET because of social stigma and
cultural beliefs that value academic paths. However, VET has offered strong job opportunities in
growing fields like healthcare and IT, where demand for skilled workers has risen significantly.
Countries with robust VET systems have shown lower youth unemployment rates. Using an
inductive approach and interpretivism philosophy, this research work has employed secondary
data collection and thematic analysis to investigate global VET trends, compare job outcomes
between vocational and degree graduates, and study successful VET models. Lastly, the
discussion section has recommended awareness campaigns and updated curriculums to shift
parental attitudes and boost VET acceptance, ensuring education has aligned with modern job
market needs.
Keywords: Vocational education, parental perception, cultural factors, employment outcomes,
social stigma, post-COVID-19, skill-based training, career choices, global trends, awareness
campaigns, inductive approach, thematic analysis.