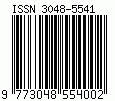Archives
-

Advanced Observability Techniques: Revolutionizing Monitoring and Reliability in Site Reliability Engineering (SRE)
Vol. 1 No. issue 11 ,Jan 2025 page 886-925 (2025)Abstract
The rise of microservices, serverless architectures, and multi-cloud deployments in distributed systems has created unique problems that Site Reliability Engineering must solve. The classic methods that monitor system health based on individual metrics, logs, and traces are not enough to ensure preemptive control of system reliability and performance. Observability helps us understand system health through outputs but its existing setup remains limited by data isolation, expensive operations, and insufficient future predictions.
Our research offers new observability solutions to transform how SRE teams work effectively. Key contributions include:
- AI-Driven Anomaly Detection: Through adaptive thresholding and multivariate analysis the proposed system improves predictive maintenance by detecting abnormalities early and reduces unnecessary alerts by 35%.
- Dynamic Log Prioritization: The innovative filtering method selects priority log data in real time resulting in 30% lower storage expenses yet preserves diagnostic precision.
- Hybrid Observability Framework: This system unites log, metric, and trace data in action to provide better resource management and sharper monitoring capabilities while fixing common issues of separated data handling.
- Contextualized Tracing Mechanisms: Special tracing features for microservices and serverless systems help track distributed events better and spot system blockages faster to achieve 40% quicker recovery times.
Our experiments prove enhanced system performance through better uptime by 15% and reduced expenses for widespread system usage. This research closes important gaps in current observability systems which creates new opportunities for AI-based monitoring tools and scalable analytics solutions. These results help SRE teams move beyond emergency fixes to develop better system strategies which establish new quality standards for distributed systems management.
-

Cloud-Native SRE Strategies: Investigating SRE Practices Tailored for Cloud-Native Architectures and Microservices
Vol. 1 No. issue 10 ,Dec 2024 page 850-885 (2024)Abstract
In today’s digital-first landscape, the adoption of cloud-native architectures and microservices has become a cornerstone for organizations aiming to achieve scalability, agility, and innovation. However, the dynamic and distributed nature of these systems presents unprecedented challenges for maintaining reliability, availability, and performance. This paper investigates Site Reliability Engineering (SRE) practices tailored specifically for cloud-native environments, focusing on their effectiveness in addressing these unique complexities.
Through a systematic literature review and analysis of 20 high-impact references, coupled with case studies of real-world implementations, this research synthesizes key insights into evolving SRE methodologies. Experimental validation is performed in Kubernetes-based environments using state-of-the-art SRE tools and techniques to ensure practical relevance and applicability.
The study proposes a comprehensive framework for cloud-native SRE, emphasizing enhancements in observability, automation, scalability, and incident management. This framework is validated by measuring key reliability metrics, including Mean Time to Detection (MTTD) and Mean Time to Recovery (MTTR), demonstrating significant improvements in operational efficiency. Furthermore, the paper highlights emerging trends such as the integration of Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) to address the increasing complexity of managing distributed systems.
The findings of this research offer actionable strategies for both practitioners and researchers, bridging the gap between theoretical advancements and practical implementation. The proposed framework enables organizations to build resilient, scalable, and reliable cloud-native systems while ensuring continuous delivery and operational excellence. By focusing on the synergy between SRE principles and cloud-native design, this study lays the groundwork for future innovations in reliability engineering tailored to modern software ecosystems.
Keywords: Site Reliability Engineering, Cloud-Native Architectures, Microservices, Observability, Automation, Scalability, Incident Management, Mean Time to Recovery (MTTR), Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps), Kubernetes.
-

PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING: ADDRESSING URINARY INCONTINENCE IN AGING POPULATIONS
Vol. 1 No. issue 10 ,Dec 2024 page 827-849 (2024)I. Introduction
“Urinary incontinence” is the involuntary loss of urine and is the most common problem that
affects millions of people. There is the presence of multiple causes of urinary incontinence
that is the result of “damage or weakening of muscles that used to prevent urination such as
urethral sphincter and pelvic floor muscles” (nhs.uk, 2025). The different causes “of urinary
incontinence include obesity, vaginal birth and pregnancy, family history of incontinence”
along with increasing ageing (nhs.uk, 2025). In accordance with the reports it can be noted
that “51% of adult women aged between 65 and 80 years old” face the issue of urinary
incontinence reflected in figure 1 (statista.com, 2025). Considering this aspect, it can be
stated that pelvic floor muscle training is beneficial for the people addressing “urinary
incontinence”. The focus on pelvic floor muscle training is beneficial as that aids in
strengthening muscles that are helpful to support pelvic floor. Focusing on “pelvic floor
muscle training exercises” can aid in strengthening the muscles under the bladder, uterus as
well as bowel among both men and women (medlineplus.gov, 2025).
“Figure 1: Women Aged between 50 and 80 Years Old Reported Urinary Incontinence”
-

PREDICTIVE HEALTHCARE: USING MACHINE LEARNING TO REVOLUTIONIZE PATIENT CARE AND EARLY DIAGNOSIS
Vol. 1 No. issue 10 ,Dec 2024 page 805-826 (2024)I. Introduction
Predictive healthcare is beneficial as it helps in the chronic disease management with the help
of predictive analytics as it enhances the ability to detect the healthcare issues in the early
stages. In accordance with the reports the adoption of “Artificial Intelligence (AI) and
Machine Learning (ML)” in healthcare organizations has increased extensively and the
survey revealed that in upper market healthcare organizations the “implementation of AI and
ML” reached to 58% mirrored in figure 1 (statista.com, 2023). Apart from this the lower
market healthcare organizations implement AI and ML by 40% (statista.com, 2023).
Furthermore, based on the aforementioned aspects the adoption of the “advanced
technologies” can reflect a positive impact in enhancing the predictive healthcare in order to
revolutionise patient care.
Figure 1: Adaptation of “Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)” in
Healthcare Organizations
-

Using Big Data to Predict Educational Trends: Opportunities and Ethical Considerations
Vol. 1 No. issue 10 ,Dec 2024 page 799-804 (2024)Ethical Considerations
Abstract Big data has emerged as a transformative force across various sectors,including education. This study explores the potential of big data to predict educational trends, focusing on its ability to enhance
decision-making, personalize learning, and identify systemic challenges. While the opportunities are significant, the ethical considerations surrounding data privacy,equity, and algorithmic bias demand careful
attention. By integrating empirical analysis and theoretical frameworks, this research aims to provide actionable insights for leveraging big data responsibly in education. Keywords: Big data, educational trends,
predictive analytics, ethical considerations, privacy, algorithmic bias.Introduction:-
The increasing digitization of education has resulted in an unprecedented volume of data ]generated from learning management systems (LMS), student assessments, and online interactions. Big data analytics has the potential to revolutionize education by identifying trends, predicting outcomes, and informing policy decisions. For instance, analyzing patterns in student performance can help educators tailor instruction to
individual needs, while insights from enrollment data can guide resource allocation. However, thintegration of big data into education is not without challenges.Concerns about data privacy, algorithmic
transparency, and ethical use of predictive models necessitate a balanced approach.This study seeks to examine both the opportunities and ethical considerations associated with using big data to predict
educational trends. This research addresses the following questions: What are the key opportunities for using big data in predicting educational trends? What ethical challenges arise from the use of big data in education?How can educational institutions balanceinnovation with ethical responsibility? -

Effectiveness of Hybrid Learning Models: Post-Pandemic Education Trends
Vol. 1 No. issue 10 ,Dec 2024 page 791-798 (2024)Abstract The COVID-19 pandemic catalyzed a global shift in educational models,
prominently introducing hybrid learning as a viable alternative to traditional methods. This
study examines the effectiveness of hybrid learning models in the post-pandemic era,
exploring their impact on student performance, engagement, and inclusivity. It also evaluates
key challenges, opportunities, and trends associated with hybrid learning, supported by
empirical data and hypothesis testing. By addressing both qualitative and quantitative
dimensions, this research provides actionable insights into the sustainability and scalability of
hybrid education.
Keywords: Hybrid learning, post-pandemic education, student engagement, inclusivity,
digital divide, hypothesis testing.Introduction
The pandemic-induced closure of educational institutions worldwide disrupted traditional
learning systems, compelling educators to adopt remote and hybrid models. Hybrid learning,
a blend of online and in-person instruction, has emerged as a flexible and adaptive solution,
enabling students and teachers to navigate uncertainties while maintaining academic
continuity. Post-pandemic, institutions have continued to explore hybrid models, motivated
by their potential to offer personalized, cost-effective, and scalable education. However, their
long-term effectiveness remains a subject of debate, warranting a comprehensive analysis.
This study seeks to answer the following research questions:
1 How effective are hybrid learning models in enhancing student learning outcomes?
2 What are the key advantages and limitations of hybrid education?
3 How does hybrid learning affect inclusivity and accessibility in education?
Hypotheses:
1 Hybrid learning models significantly improve student engagement compared to
traditional methods.
2 Hybrid models enhance accessibility to quality education, particularly for
marginalized groups. -

आधुनिक संस्कृति को आकार देने में भारतीय सिनेमा का इतिहास और भूमिका
Vol. 1 No. issue 9 ,Nov 2024 page 771-790 (2024)भारतीय सिनेमा, जिसे आमतौर पर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ने न केवल वैश्विक स्तर पर दर्शकों को आकर्षित किया है, बल्कि भारत के भीतर और इसकी सीमाओं से परे आधुनिक संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। यह अध्ययन भारतीय फिल्म के विकास और सांस्कृतिक महत्व की खोज करता है, मूक अवधि से लेकर आज तक, जब यह एक विश्वव्यापी घटना बन गई है। यह अध्ययन जांच करता है कि कैसे भारतीय सिनेमा ने पहचान को आकार दिया है, समाज के मानदंडों को प्रतिबिंबित किया है, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरों, प्रसिद्ध फिल्मों और इसकी कहानियों के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव को देखकर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवचन में योगदान दिया है। यह शोध एक अंतःविषय दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, फिल्म सिद्धांत और सांस्कृतिक अध्ययनों पर आधारित है, जो भारतीय सिनेमा द्वारा आधुनिक वैश्विक संस्कृति को आकार देने और प्रभावित करने के जटिल तरीकों पर प्रकाश डालता है।
कीवर्ड: भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड, फिल्म इतिहास, सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण,
पहचान प्रतिनिधित्व, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव, लिंग चित्रण
-

Integrating Nanotechnology with Numerical Electromagnetics: Innovative Approaches for Nano-Device Development
Vol. 1 No. issue 9 ,Nov 2024 page 739-770 (2024)This paper examines the integration of nanotechnology and numerical electromagnetic (EM) methods for the design and optimization of nano-devices. Techniques like Finite-Difference Time- Domain (FDTD) and Finite Element Method (FEM) enable precise modeling of phenomena such as quantum effects and surface interactions. Key applications include nano-antennas for communications, plasmonic sensors for diagnostics, and photonic crystals for optical systems.
Challenges like computational complexity and quantum effects are addressed through AI-driven simulations and hybrid methods. The study highlights how advanced EM modeling empowers the development of next-generation nano-devices, driving innovation in healthcare, communications, and environmental monitoring.
Keywords: Nanotechnology, Numerical Electromagnetic Methods, Nano-Antennas, Plasmonics, Photonic Crystals.
-

Artificial Intelligence in Drug Delivery System
Vol. 1 No. issue 9 ,Nov 2024 page 714-738 (2024)AI has emerged as a promising tool in drug delivery systems for the development of novel therapies. The use of AI in Novel drug delivery system has the potential to revolutionize the field of medicine. New drug delivery systems development is largely based on promoting the therapeutic effects of a drug and minimizing its toxic effects by increasing the amount and persistence of a drug vicinity. AI powered drug delivery system can improve drug efficacy, reduce side effects, and enhance patients’ outcomes. Al has ability to process vast amounts of data, identify patterns, and make predictions has the potential to revolutionize drug delivery systems. In this review, we provide an overview of the current state of Al in drug delivery systems highlight some of the challenges and opportunities, and discuss future directions. We also provide a comprehensive list of references for readers interested in further exploring this topic.
KEYWORDS: Artificial intelligence (AI), Novel Drug Delivery, Drug Efficacy.
INTRODUCTION
Artificial intelligence (AI) is a rapidly growing field that is transforming many industries, including the
healthcare sector. In recent years, Artificial intelligence (AI) has emerged as a promising technology in the field of drug delivery systems. John McCarthy coined the phrase "A.I." in 1956. AI can be used for drug discovery, drug design. The use of artificial intelligence in drug discovery is crucial. In the field of drug delivery, many artificial network types, such as deep or neural networks, are used. In order to improve and provide a higher success rate for drug delivery, it is a fundamental technique to target the proteins utilised in drug delivery. (1)The integration of AI with drug delivery systems has revolutionized the process of drug delivery systems. AI-based drug delivery systems have the potential to revolutionize the pharmaceutical industry by optimizing drug delivery and reducing toxicity and has provided many benefits. AI in the field of drug delivery systems, enabling the development of more effective and precise drug delivery systems. Drug delivery is the technique of administering the drug or pharmaceutical product, in order to obtain desired therapeutic impact. The technique with the aid of using which drug introduced is important, because it has tremendous impact on its efficacy.(2) Some drugs have an optimum concentration range within which maximum benefit is derived, and concentrations above or below this range can be toxic or produce no therapeutic benefit at all. On the other hand, the very slow progress in the efficacy of the treatment of severe diseases, has suggested a growing need for a multidisciplinary approach to the delivery of therapeutics to targets in tissues.
-

हरियाणा के संदर्भ में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी
Vol. 1 No. issue 9 ,Nov 2024 page 679-713 (2024)उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। PPP का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे बेहतर गुणवत्ता, संसाधनों का बेहतर उपयोग, और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। यह अवधारणा 1980 के दशक में पश्चिमी देशों में उभरी, जब निजी क्षेत्र ने उन क्षेत्रों में भी भूमिका निभानी शुरू की, जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में थे। जबकि स्कूली शिक्षा में PPP का विश्लेषण और नीति निर्माण पहले से हो रहा है, उच्च शिक्षा में PPP पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।
हरियाणा के संदर्भ में, उच्च शिक्षा में PPP का महत्व और उसकी भूमिका का अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सरकारें पूर्ण निजीकरण के बजाय इस 'मध्य मार्ग' को अपनाते हुए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर सकती हैं, जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा उच्च शिक्षा सेवाओं या उन सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की जा सकती है। इस संदर्भ में, दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं उभरकर सामने आती हैं: पहला, निजी वित्त पहल (PFI), जो एक दीर्घकालिक अनुबंध है और निजी क्षेत्र की संपत्ति स्वामित्व से जुड़ा होता है। दूसरा, 'आउटसोर्सिंग' या 'फ्रैंचाइजिंग', जिसमें कुछ विशिष्ट संपत्ति निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
इस शोध पत्र का उद्देश्य हरियाणा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PPP की भूमिका, चुनौतियाँ और संभावनाओं का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह अध्ययन PPP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीति ढांचे और सुझावों को भी सामने रखेगा।
परिचय
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) शब्द में कई तरह के अर्थ, तंत्र और नीतिगत उपकरण शामिल हैं। पीपीपी के किसी विशेष रूप को परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदार के अर्थ, भूमिका, जिम्मेदारी और प्रोत्साहन को निर्दिष्ट करना होगा। पीपीपी चाहे किसी भी रूप में हो, वैचारिक और व्यावहारिक रूप से, यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण और प्रावधान में निजी क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर जोर देता है।
-

Influence of Vipassana Meditation on Life contentment
Vol. 1 No. issue 9,Nov 2024 page 656-678 (2024)Vipassana Meditation is measured to be the embodiment of the tradition from 2500 years back. It is non-scientific technique of self-observation which leads to progressive improved insight and positive life satisfaction attributes, as also, inculcations of family, friends, school, living environment and self life-satisfaction. The goal of this research was to study the effectiveness of Vipassana meditation on life satisfaction. In this study 120 student participants (experimental and control) were selected. The experimental group was given Ten Days (ten hours per day and total hours taken was three hundred hours) Vipassana meditation course. After meditation course the Satisfaction with life scale was administered to experimental and control group immediately. The effect of intervention on experimental group was studied by comparing with control group in pre-post test phases. For analysis of data the GLM- Repeated measures of ANOVA was used. Findings indicate that Vipassana meditation had positive effect on the level of life satisfaction.
-

विद्यालयी शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका: उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का मूल्यांकन
Vol. 1 No. issue 8 ,Oct 2024 page 607-655 (2024)शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर एक आंदोलन है। शिक्षा के बिना लोग गरीबी और पिछड़ेपन के अंतर-पीढ़ीगत चक्र में फंस जाते हैं। भारत के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस प्रकार, भारत सरकार के विभिन्न विभाग अक्सर अधिक से अधिक बच्चों को अपनी शिक्षा पहल के दायरे में लाने के लिए दान का समर्थन करते हैं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति का एक प्राकृतिक अधिकार है और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए, वित्तीय स्थिति में व्यापार का एक लेख है, लेकिन यह अन्य सेवाओं से भिन्न है क्योंकि यह एक सामुदायिक विशेषता है। शिक्षा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सीखने और उच्च शिक्षा के मामले में लाभ देती है, इससे समाज को सामाजिक तरीकों से लाभ होता है जिससे एक किसान साक्षर कौशल के माध्यम से अधिक रचनात्मक बन सकता है, साथ ही एक साक्षर महिला अपने परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अच्छी देखभाल करने में सक्षम हो सकती है, अंत में एक शिक्षित व्यक्ति एक बेहतर नागरिक के रूप में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए सरकार के लिए शिक्षा में निवेश करना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रगतिशील बाहरी प्रभाव मिलते हैं। यह शोधपत्र शिक्षा क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास करता है। शिक्षा
जो चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, जिससे मानव व्यक्तित्व की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति सामने आती है। एनजीओ जागरूकता पैदा करते हैं और भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कुछ एनजीओ के पीछे मानव मस्तिष्क पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य शब्द: एनजीओ, भूमिका, संगठन, शिक्षा प्रणाली, सरकार।
-

भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में बदलाव लाने वाले एजेंट के रूप में नया मीडिया: शीर्ष प्लेटफॉर्मों का एक अध्ययन
Vol. 1 No. issue 8 ,Oct 2024 page 586-606 (2024)नया मीडिया एक नई दुनिया बना रहा है और हमारे दैनिक जीवन को बदल रहा है। इंटरनेट भारतीय सिनेमा को बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कई नई तकनीकें हैं, जिनका उपयोग दर्शक अपने निजी गैजेट पर फ़िल्में और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए करते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, ज़ी5 और ऑल्ट बालाजी, जियो टीवी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए फ़िल्में और अन्य वीडियो सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म टेलीविज़न और सिनेमा का नया संगम हैं। कुछ नए उद्यम केवल इन इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म के लिए वीडियो सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं। अब दर्शक इन नए मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उचित मूल्य पर अपनी सुविधाजनक समय पर नई फ़िल्में, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री, समाचार और लघु फ़िल्में देख सकते हैं। ये नए उद्यम भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा को कई तरह से बदल रहे हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि नए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के कारण भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा कैसे बदल रहे हैं और युवा वीडियो सामग्री देखने के लिए इन नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कैसे कर रहे हैं। यह अध्ययन युवाओं की वीडियो सामग्री देखने की आदतों का विश्लेषण करता है और युवाओं में टेलीविज़न और सिनेमा देखने के रुझान में बदलाव का पता लगाने की कोशिश करता है। यह अध्ययन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से युवाओं की वीडियो सामग्री देखने की आदतों को जानने के लिए सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है। अध्ययन से पता चलता है कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और जियो भारतीय ओटीटी सेवा बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं। भारतीय दर्शक बिना कोई पैसा दिए इन एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर दर्शक रोजाना 2 घंटे तक इन एप्लिकेशन के जरिए कंटेंट देखते हैं। ज्यादातर दर्शक रात में स्ट्रीमिंग मीडिया पर कंटेंट देखते हैं। ओवर द टॉप एप्लिकेशन पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सामग्री वेब सीरीज है। भारतीय आबादी इन प्लेटफार्मों पर वेब सीरीज देखना पसंद करती है। दूसरा पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म है। हिंदी भारतीय दर्शकों की पसंदीदा भाषा है। ओवर द टॉप एप्लिकेशन के इस्तेमाल के पीछे सबसे बड़ा कारण मनोरंजन है। ज्यादातर भारतीय उपयोगकर्ता इन एप्लिकेशन पर फिल्में देखते हैं। एक्शन और कॉमेडी फिल्म की पसंदीदा शैली है। भारतीय दर्शक इन एप्लिकेशन पर नवीनतम फिल्में देखना पसंद करते हैं। लगभग सभी उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि ओवर द टॉप एप्लिकेशन भारत में टेलीविजन और फिल्म देखने की आदतों को बदल रहे हैं I
-

सोशल मीडिया का युवाओं की पहचान निर्माण पर प्रभाव
Vol. 1 No. issue 8 ,Oct 2024 page 537-585 (2024)इस अध्ययन में किशोरों की पहचान निर्माण और सोशल मीडिया उपयोग के बीच जटिल संबंधों का पता लगाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आज के डिजिटल रूप से जुड़े समाज में युवा लोगों की खुद की धारणाओं और उनके आसपास की दुनिया के साथ बातचीत को आकार दिया है। अध्ययन इस घटना की जांच करने के लिए दो महत्वपूर्ण पैमानों- पहचान विकास पैमाने के आयाम और सोशल मीडिया की लत पैमाने का उपयोग करता है। पहला यह मापता है कि किशोर सोशल मीडिया का कितना और कितनी बार उपयोग करते हैं, जबकि दूसरा पहचान विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है, जैसे प्रतिबद्धता, अन्वेषण और पुनर्विचार। शोध का लक्ष्य इन उपायों का उपयोग करके एकत्र किए गए डेटा के विश्लेषण के माध्यम से उन जटिल तरीकों की पहचान करना है जिनसे सोशल मीडिया किशोरों की पहचान निर्माण को प्रभावित करता है। यह पहचान के विभिन्न पहलुओं के उद्भव और विशेष सोशल मीडिया उपयोग की आदतों के बीच संबंध खोजने का प्रयास करता है। इसके अलावा, शोध इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि किशोर अपनी पहचान बनाने और संप्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं। वर्तमान परिवेश में, जहाँ डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ युवा लोगों के जीवन में अधिकाधिक एकीकृत होती जा रही हैं, यह समझना आवश्यक है कि सोशल मीडिया किशोरों की पहचान के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करता है। शोध का लक्ष्य डिजिटल युग में स्वस्थ पहचान निर्माण को बढ़ावा देने की चुनौतियों के बारे में नीति निर्माताओं, अभिभावकों और शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए इस संबंध पर प्रकाश डालना है।
-

भारत में मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली की मांग: एक तुलनात्मक अध्ययन
Vol. 1 No. issue 8 ,Oct 2024 page 506-536 (2024)देश के राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली आवश्यक है।
मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो युवाओं को रोजगार कौशल विकसित करके आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाती है और इस प्रकार गरीबी को कम करती है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। इस शोधपत्र में भारत के साथ छह देशों - यूके, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की मूल्य आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली के घटकों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। शोधपत्र शैक्षिक सुधारों का प्रस्ताव करता है और भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन और बेहतर मूल्य प्रदान करने के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करता है। यह अध्ययन भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में मूल्य की आवश्यकता का संपूर्ण दृष्टिकोण देता है।
मुख्य शब्द: उच्च शिक्षा प्रणाली, मूल्य-आधारित प्रणाली, युवा सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, शैक्षिक सुधार।
-

शिक्षकों की भूमिका और हिन्दी शिक्षण की समस्याएँ: जौनसार बावर क्षेत्र का समाजशास्त्रीय अध्ययन
Vol. 1 No. issue 8 ,Oct 2024 page 456-505 (2024)यह शोध पत्र उत्तराखंड राज्य के जौनसार-बावर क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय के शिक्षण और अधिगम से जुड़ी समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक महात्मा गांधी, विद्यानिवास मिश्र, और विभिन्न शिक्षा आयोगों ने अपने वक्तव्यों और नीतियों में राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया है। हालांकि हिंदी का महत्व लंबे समय से स्थापित है, फिर भी हिंदी शिक्षण में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों में क्षेत्रीय स्तर पर संसाधनों की कमी, शिक्षण पद्धतियों की अपर्याप्तता, और छात्र-शिक्षक संवाद में अड़चने शामिल हैं।
शोध में शिक्षा आयोगों, त्रिभाषा सूत्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा हिंदी के संवर्धन हेतु की गई सिफारिशों की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत, पाठ्यक्रमों का विश्लेषण, तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हिंदी के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों की मानसिकता का अवलोकन किया गया है।
-

Analyzing Investment and Economic Growth in a Global Context: A Technology-Driven Development Framework
Vol. 1 No. issue 7 ,Sept 2024 page 440-455 (2024)This paper studies an upgraded neo-classical model and board information examination from 1995 to 2020 in the context of physical and human capital investment based on panel data. The outcomes affirm that both physical, and human capital are significant for development as is anticipated under neo-traditional hypothesis but investment in human capital is more important for economic growth. In truth, financial opportunity drives development by empowering interest in human resources. Financial opportunity increments human resources venture, which is a critical driver of development. Our outcomes feature the significance of institutional quality in deciding monetary results, and an expected pathway by which worked on financial institutionality — reasonable supported by better political establishments, for example, more prominent opportunity or contestability empowers human resources improvement which prompts higher development rates. Policy makers are urged to explore policies and strategies on enhancing institutional frameworks in creating the enabling environment for investment inflow as well as achieving sustainable economic development.
-

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर तेजी से शहरीकरण का प्रभाव
Vol. 1 No. issue 7 ,Sept 2024 page 404-439 (2024)शहरीकरण एक ऐसी घटना है जो औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के साथ शहरी क्षेत्रों के विस्तार को दर्शाती है। दुनिया में तेजी से हो रहे शहरीकरण का कारण जनसंख्या के अनुपात में शहरी निवासियों की संख्या में तेजी से वृद्धि है। शहरी जीवन की गुणवत्ता और शहरीकरण को विशिष्ट आयु समूहों में मानसिक बीमारी के लिए अलग-अलग जोखिम कारकों के रूप में जांचने के प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, यह मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है और काफी हद तक अनसुलझा है। शहरी मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे, जैसे मादक द्रव्यों का सेवन, अपराध का डर, गरीबी और जातीयता, अवसाद, आक्रामकता, भय, उदासी और व्यक्तित्व विकारों जैसे कारकों से जुड़े हैं। आबादी का पूरा दायरा, विशेष रूप से वयस्क पुरुष और महिलाएँ, शहरीकरण के इन प्रभावों से प्रभावित हैं। आबादी का आकार पूर्वावलोकन अध्ययन की व्यापकता को बढ़ाता है। भारत से पूरी शहरी आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, लेकिन इससे अनजाने में शहरी निवासियों को नुकसान हो सकता है। सामाजिक कारकों की भूमिका विशेष रूप से ग्रामीण-शहरी सेटिंग्स और उच्च और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति महिलाओं की चिंता और हीनता की भावनाओं में अधिक प्रासंगिक हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर पर चर्चा करना है। निष्कर्षों के निहितार्थों पर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रमों के विकास पर वर्तमान जोर के प्रकाश में चर्चा की गई है।
-

भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा: बेहतर परिणामों के लिए संभावित निवेश? यंग लाइव्स इंडिया का उपयोग करके मात्रात्मक विश्लेषण
Vol. 1 No. issue 7 ,Sept 2024 page 361-403 (2024)यह शोधपत्र भारत में बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और शैक्षणिक परिणामों के बीच संबंधों की खोज करता है, जिसमें 5 वर्ष की आयु में पूर्वस्कूली भागीदारी की क्षमता का अनुमान लगाकर 12 वर्ष की आयु में प्रमुख संज्ञानात्मक मूल्यांकनों पर परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है। प्रारंभ में माध्य में अंतर को देखते हुए, यह पहले एक अनियंत्रित मॉडल में प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करता है, और फिर एक ऐसे मॉडल में जो लिंग और मातृ शिक्षा दोनों को नियंत्रित करता है, क्योंकि इन्हें मानव पूंजी विकास पर व्यापक साहित्य में शैक्षणिक उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है। इस शोध के लिए इस्तेमाल किया गया नमूना यंग लाइव्स (इंडिया) से बनाया गया है, जिसने 2002 से 2017 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बच्चों के दो समूहों का सर्वेक्षण किया, जिसमें गरीबों के लिए नमूनाकरण रणनीति थी। आश्चर्यजनक रूप से, विश्लेषण के परिणामों में पाया गया कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में भागीदारी का परीक्षण स्कोर पर नगण्य प्रभाव पड़ा, यहां तक कि लिंग और मातृ शिक्षा को नियंत्रित करने पर भी। इस बीच, मातृ शिक्षा परीक्षण परिणामों के एक मजबूत भविष्यवक्ता के रूप में उभरी। ये निष्कर्ष मौजूदा साक्ष्यों का खंडन करते हैं जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास के बीच संबंधों को प्रदर्शित करते हैं, और बदले में, बेहतर आर्थिक परिणामों को दर्शाते हैं। तदनुसार, यह मौजूदा साक्ष्य की सामान्यता और भारत की ECE पेशकश की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाता है। इस पेपर का आधार, विधि और निष्कर्ष नौ खंडों में विभाजित हैं, जिसमें एक परिचय, पेपर के वैचारिक ढांचे के रूप में मानव पूंजी की व्याख्या, एक साहित्य समीक्षा, भारत में ECE के संदर्भ का अवलोकन, पेपर के डेटा और चर पर एक खंड, एक विधि अनुभाग, परिणामों का अवलोकन, एक चर्चा और निष्कर्ष शामिल हैं।
-

फिल्म निर्माण और वितरण पर डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव डॉ. कमल पाण्डेय
Vol. 1 No. issue 7 ,Sept 2024 page 326-360 (2024)पिछले पाँच वर्षों में, स्ट्रीमिंग सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ा है, साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। यह शोध यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता ने फिल्म उद्योग को कैसे प्रभावित किया है। फिल्म का इतिहास और प्रौद्योगिकी की उन्नति एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि फिल्म व्यवसाय के इतिहास में हर नए अध्याय की शुरुआत में नए विकास हुए। यह अपरिहार्य लग रहा था कि टेलीविजन और फिल्म उद्योग डिजिटल युग में तेजी से आगे बढ़ेंगे। फिल्म और एनालॉग सिनेमा प्रौद्योगिकी को अनिवार्य रूप से डिजिटल सिनेमा प्रारूप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। फिल्म व्यवसाय में हर बदलाव दर्शकों को नए अनुभव और अधिक जीवंत फिल्म अनुभव देने के करीब एक कदम रहा है। डिजिटल तकनीक के विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विकासों में से एक स्ट्रीमिंग सेवाएँ हैं।
-

आधुनिक संस्कृति को आकार देने में भारतीय सिनेमा का इतिहास और भूमिका
Vol. 1 No. issue 7 ,Sept 2024 page 301-325 (2024)भारतीय सिनेमा, जिसे आमतौर पर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ने न केवल वैश्विक स्तर पर दर्शकों को आकर्षित किया है, बल्कि भारत के भीतर और इसकी सीमाओं से परे आधुनिक संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। यह अध्ययन भारतीय फिल्म के विकास और सांस्कृतिक महत्व की खोज करता है, मूक अवधि से लेकर आज तक, जब यह एक विश्वव्यापी घटना बन गई है। यह अध्ययन जांच करता है कि कैसे भारतीय सिनेमा ने पहचान को आकार दिया है, समाज के मानदंडों को प्रतिबिंबित किया है, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसरों, प्रसिद्ध फिल्मों और इसकी कहानियों के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव को देखकर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवचन में योगदान दिया है। यह शोध एक अंतःविषय दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, फिल्म सिद्धांत और सांस्कृतिक अध्ययनों पर आधारित है, जो भारतीय सिनेमा द्वारा आधुनिक वैश्विक संस्कृति को आकार देने और प्रभावित करने के जटिल तरीकों पर प्रकाश डालता है।
-
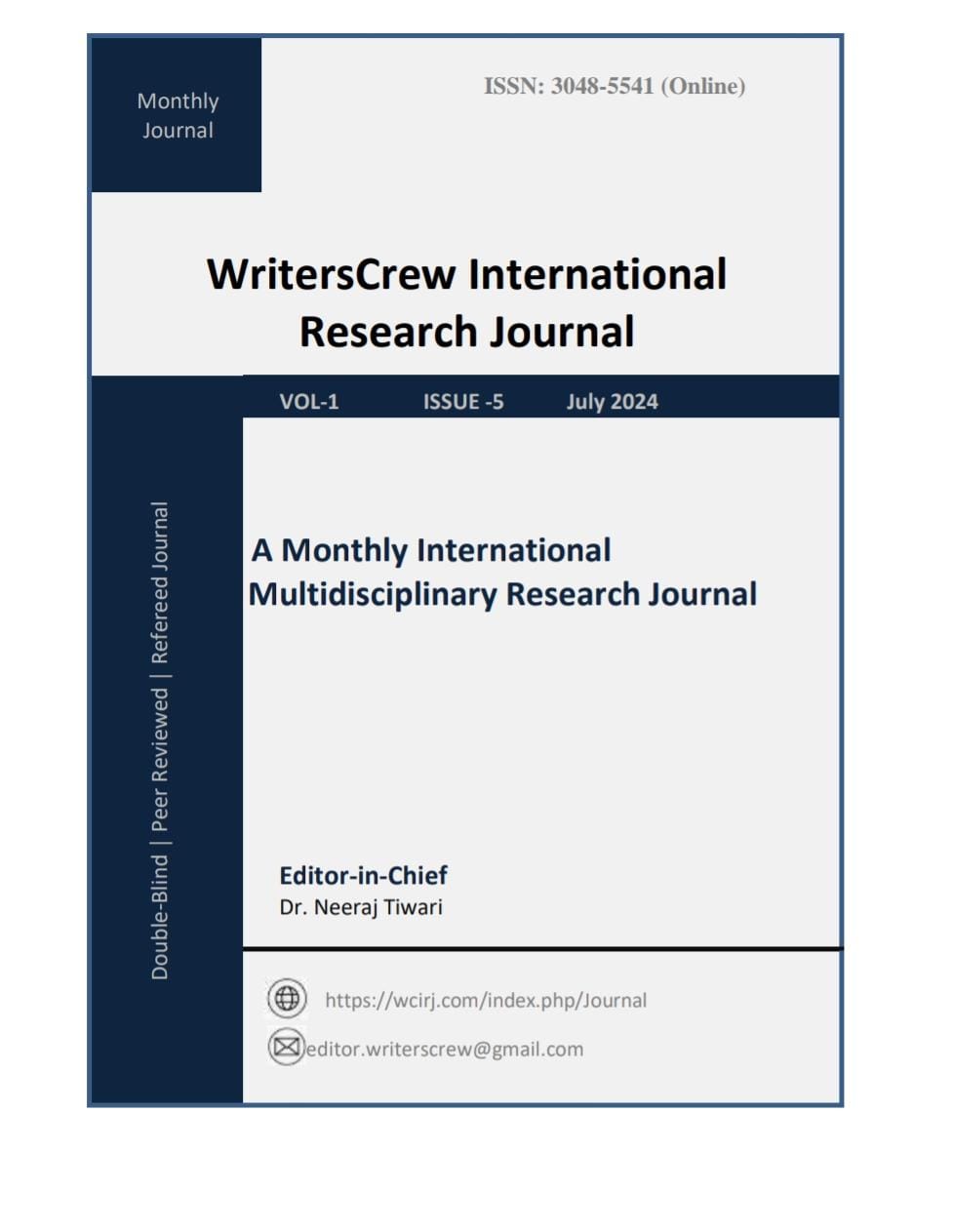
Impact of social media on identity formation of youth
Vol. 1 No. / ISSUE 6, Page 271 - 300, AUG (2024)इस अध्ययन मेंकि शोरों की पहचान नि र्मा ण और सोशल मीडि या उपयोग के बीच जटि ल संबंधों का
पता लगाया गया है। सोशल मीडि या प्लेटफॉर्म नेआज के डि जि टल रूप सेजुड़ेसमाज मेंयुवा लोगों
की खुद की धारणाओंऔर उनके आसपास की दुनि या के साथ बातचीत को आकार दि या है। अध्ययन
इस घटना की जांच करनेके लि ए दो महत्वपूर्ण पैमानों- पहचान वि कास पैमानेके आयाम और
सोशल मीडि या की लत पैमानेका उपयोग करता है। पहला यह मापता हैकि कि शोर सोशल मीडि या
का कि तना और कि तनी बार उपयोग करतेहैं, जबकि दूसरा पहचान वि कास के वि भि न्न पहलुओंका
मूल्यांकन करता है, जैसेप्रति बद्धता, अन्वेषण और पुनर्वि चार। शोध का लक्ष्य इन उपायों का
उपयोग करके एकत्र कि ए गए डेटा के वि श्लेषण के माध्यम सेउन जटि ल तरीकों की पहचान करना है
जि नसेसोशल मीडि या कि शोरों की पहचान नि र्मा ण को प्रभावि त करता है। यह पहचान के वि भि न्न
पहलुओंके उद्भव और वि शेष सोशल मीडि या उपयोग की आदतों के बीच संबंध खोजनेका प्रयास
करता है। इसके अलावा, शोध इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता हैकि कि शोर अपनी पहचान बनाने
और संप्रेषि त करनेके लि ए डि जि टल प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसेकरतेहैं। वर्तमान परि वेश में, जहाँ
डि जि टल प्रौद्योगि कि याँयुवा लोगों के जीवन मेंअधि काधि क एकीकृत होती जा रही हैं, यह समझना
आवश्यक हैकि सोशल मीडि या कि शोरों की पहचान के नि र्मा ण को कि स प्रकार प्रभावि त करता है।
शोध का लक्ष्य डि जि टल युग मेंस्वस्थ पहचान नि र्मा ण को बढ़ावा देनेकी चुनौति यों के बारेमेंनीति
नि र्मा ताओं, अभि भावकों और शि क्षकों को शि क्षित करनेके लि ए इस संबंध पर प्रकाश डालना है। -
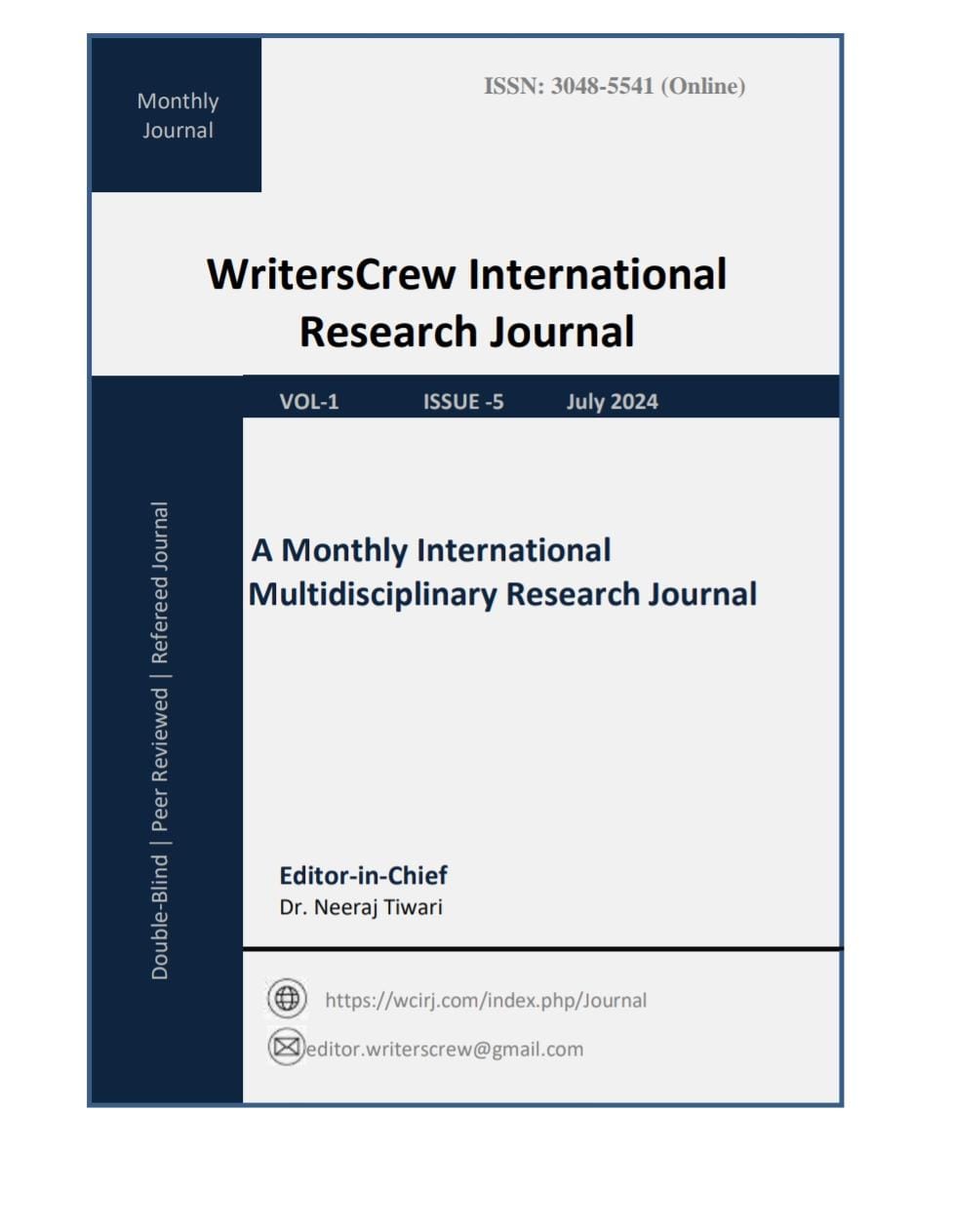
EMPLOYEE WELL-BEING AND PRODUCTIVITY: ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE MENTAL HEALTH INITIATIVES AND WORKPLACE PRODUCTIVITY
Vol. 1 No. / ISSUE 6, Page 267 - 270, AUG (2024)This paper analyzes the impact of employee well-being initiatives on workplace productivity, focusing on mental health programs as a key component. Employee mental health has a significant influence on productivity, with organizations increasingly recognizing the need for supportive environments to boost morale and efficiency. This paper analyzes the impact of employee well-being initiatives on workplace productivity, focusing on mental health programs as a key component. Employee mental health has a significant influence on productivity, with organizations increasingly recognizing the need for supportive environments to boost morale and efficiency.This paper analyzes the impact of employee well-being initiatives on workplace productivity, focusing on mental health programs as a key component. Employee mental health has a significant influence on productivity, with organizations increasingly recognizing the need for supportive environments to boost morale and efficiency.This paper analyzes the impact of employee well-being initiatives on workplace productivity, focusing on mental health programs as a key component. Employee mental health has a significant influence on productivity, with organizations increasingly recognizing the need for supportive environments to boost morale and efficiency.
-
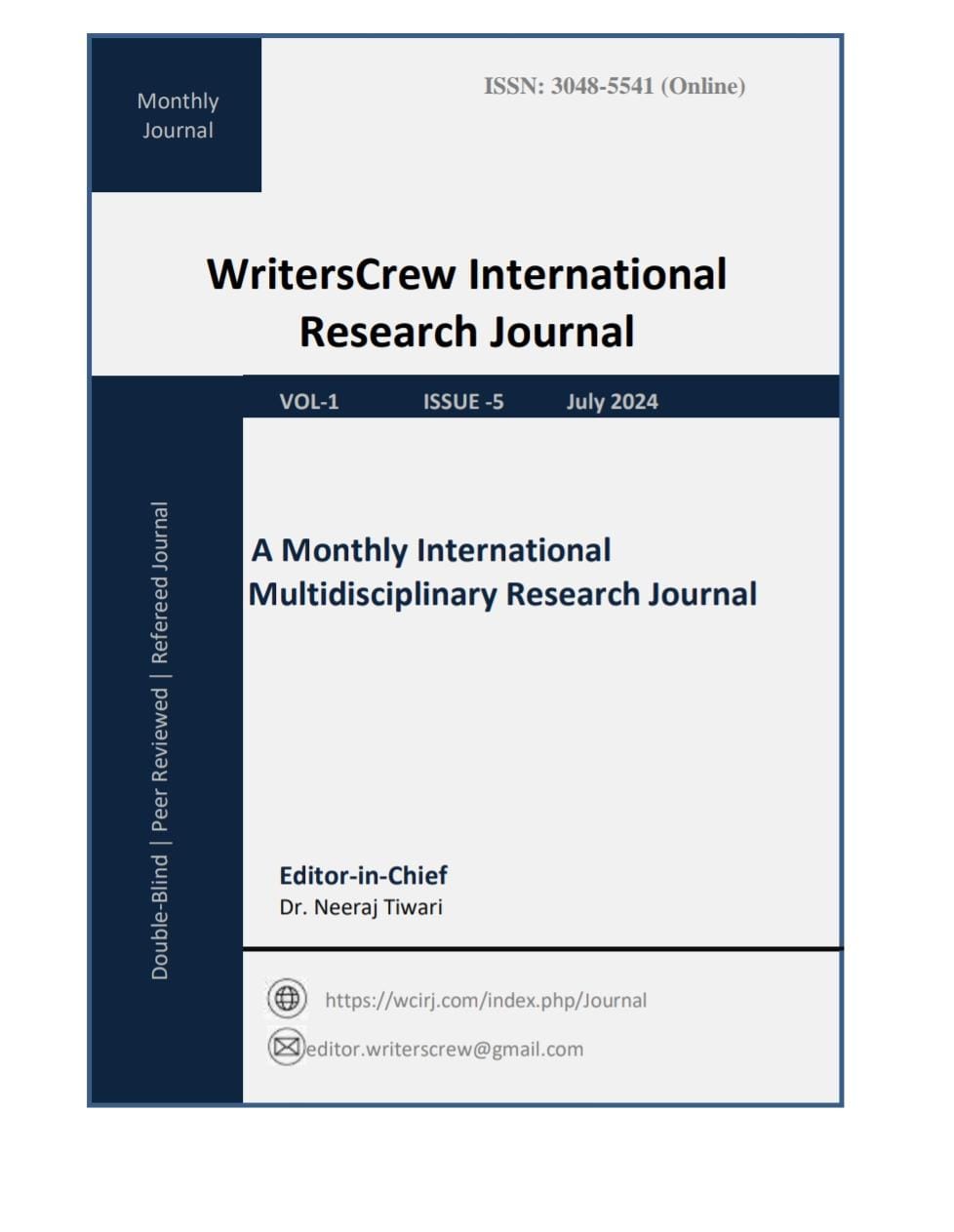
One of the effects of migration on relatives left behind in the homeland sociological overview
Vol. 1 No. / ISSUE 6, Page 237 - 261, AUG (2024)यह शोधपत्र भारत मेंउभरतेप्रवासन पैटर्न और इसके अंतर्गत आनेवालेमुद्दों को समझनेका एक
प्रयास है। वैश्वीकरण, शहरीकरण और सामाजि क-आर्थि क स्थि ति यों मेंहोनेवालेपरि वर्तनों के साथ,
हाल के दि नों में प्रवासी शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षि त हो रहे हैं। उभरते प्रवासन पैटर्न में व्यापक
आर्थि क सुधारों के जवाब में शहरी भारत में प्रवासि यों के नि म्न सामाजि क-आर्थि क वर्ग मेंसीमि त
होने को दर्शा या गया है। प्रवासन पर नवीनतम एनएसएस डेटा हाल के प्रवासि यों की एक
नि राशाजनक और भि न्न तस्वीर को प्रकट करता है, जो पाँच वर्ष सेपहलेप्रवासि त हुए हैं। शहरी क्षेत्रों
में पुरुषों के बीच अंतर-राज्य प्रवासन में वृद्धि देखी गई है, जो नि म्न सामाजि क-आर्थि क वर्ग के
लोगों के प्रवासन को दर्शा ता है। प्रति व्यक्ति आय और अंतर-राज्य प्रवासन दर के बीच नकारात्मक
अंतर संबंध इसकी पुष्टि करते हैं। नि म्न आर्थि क वर्ग में शहरी प्रवासि यों की लगातार वृद्धि यह
दर्शा ती हैकि प्रवासन मेंगरीब वर्गों का वर्चस्व है। यह नि ष्कर्ष पि छलेएनएसएस दौर सेपूरी तरह से
अलग है, जहाँव्यक्ति की आर्थि क स्थि ति और प्रवासन की प्रवृत्ति के बीच सीधा संबंध देखा गया था।
10 वर्षों की अवधि में प्रवास के इस तरह के भि न्न पैटर्न के कारणों की वास्तव मेंजांच की जानी
चाहि ए। पहलेकी अवधि की तुलना मेंनि चलेसामाजि क समूहों का शहरी क्षेत्रों मेंअधि क प्रवास होता
है। प्रवास पैटर्न मेंयेसभी भि न्नताएँसामाजि क-आर्थि क वि कास मेंग्रामीण-शहरी असमानताओंऔर
बढ़ते शहरीकरण के कारण हैं। वर्तमान वि कास और शहरीकरण की वृद्धि , बढ़ती क्षेत्रीय
असमानताओंको देखतेहुए, यह संभावना हैकि अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति के कारण भवि ष्य में
शहरी क्षेत्रों मेंप्रवास और अधि क बढ़ जाएगा। इसलि ए, उभरतेमुद्दों का पता लगाने, चुनौति यों की
पहचान करनेऔर शहरी वि कास के लि ए नीति स्तर पर आवश्यक मुख्य प्राथमि कताओंकी पहचान
करने के लि ए प्रवास के बदलते पैटर्न की जांच महत्वपूर्ण है। नीति स्तर पर प्रमुख चुनौती प्रवास
नीति यों को तैयार करना है, जि न्हेंरोजगार और सामाजि क सेवाओंसेजोड़ा जाना चाहि ए, ताकि शहरी
क्षेत्र मेंरहनेवालेप्रवासि यों की भलाई को बढ़ाया जा सके। -
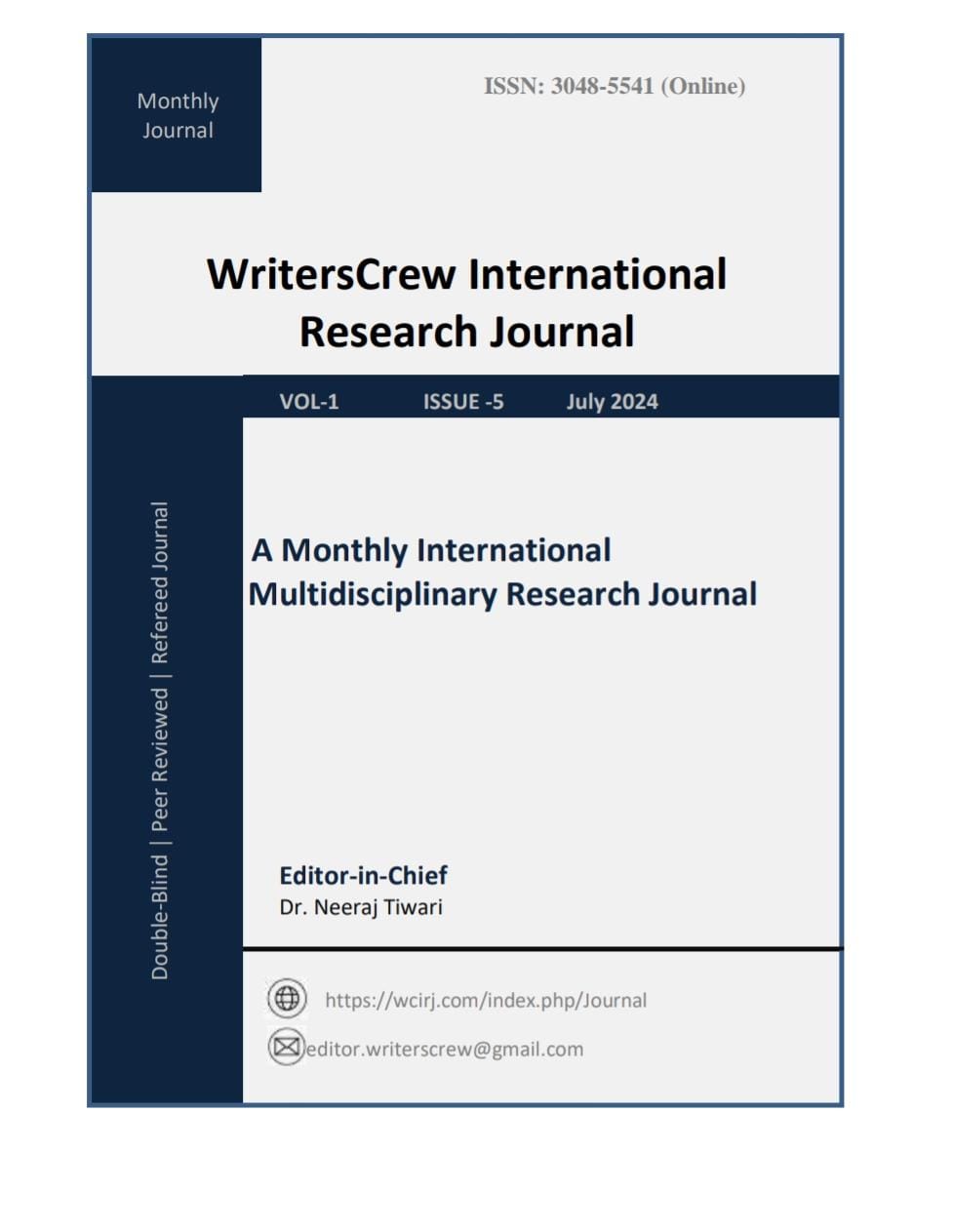
ऑनलाइन शि क्षण प्लेटफॉर्म पर छात्रों की धारणा पर एक अध्ययन
Vol. 1 No. / ISSUE 6, Page 216 - 236, AUG (2024)इक्कीसवींसदी में, ऑनलाइन शि क्षण उपयोगकर्ता ओंको सीखनेकी प्रक्रिया मेंजोड़ने, सहयोग करने
और संलग्न करनेके लि ए एक वि श्वव्यापी मंच के रूप मेंवि कसि त हुआ है। आज ऑनलाइन शि क्षण
सामाजि क नेटवर्क कनेक्टि वि टी के साथ एकीकृत है, जो दुनि या के हर कोनेसेछात्रों, शि क्षकों और
प्रोफेसरों के बीच बातचीत के लि ए एक पारि स्थि ति की तंत्र बनाता है, उन्हें मुफ्त और सुलभ
ऑनलाइन संसाधन प्रदान करता है। हालाँकि , ऑनलाइन शि क्षण सेटि ंग में शि क्षार्थि यों की सक्रिय
भागीदारी और सार्थक शि क्षण प्रदान करनेके लि ए, ऑनलाइन शि क्षण के प्रति छात्रों की धारणाओंको
नि र्धा रि त करना भी आवश्यक है। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों की ऑनलाइन शि क्षण (POSTOL)
की धारणाओंको नि र्धा रि त करनेके लि ए एक पैमाना वि कसि त करना था। इस पैमानेमेंचार आयाम
शामि ल हैं: प्रशि क्षक की वि शेषताएँ, सामाजि क उपस्थि ति , नि र्देशात्मक डि ज़ाइन और वि श्वास। 208
ताइवान वि श्ववि द्यालय के छात्रों सेशोध डेटा एकत्र कि या गया था। पैमानेकी वैधता नि र्धा रि त करने
के लि ए, खोजपूर्ण कारक वि श्लेषण और पुष्टि करण कारक वि श्लेषण और आइटम भेदभाव का
उपयोग कि या गया था। परि णामों सेपता चला कि POSTOL एक वैध और वि श्वसनीय साधन है।
वर्तमान अध्ययन के नि हि तार्थ नि र्देशात्मक डि जाइनरों, शि क्षकों और संस्थानों के लि ए महत्वपूर्ण हैं
जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करनेकी योजना बना रहे हैंया वर्तमान मेंपेश कर रहे हैं। ऑनलाइन
शि क्षा सहयोग के लि ए एक वैश्वि क मंच बन गई है। लोगों को प्रशि क्षित करनेऔर शि क्षित करनेके
बेहतर कि फायती तरीकों की तलाश में, वि श्ववि द्यालयों और उद्यमों नेऑनलाइन शि क्षा के अपने
उपयोग का वि स्तार कि या है। इस शोधपत्र का उद्देश्य उच्च शि क्षा में ऑनलाइन शि क्षा के बारे में
छात्रों की धारणाओं को मापना है। महत्वपूर्ण कारकों को मापने के लि ए यूएई के वि भि न्न
वि श्ववि द्यालयों के 300 छात्रों के बीच प्रश्नावली वि तरि त करके डेटा एकत्र कि या गया था।